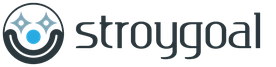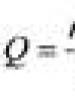गायत्री मंत्र शुद्धि एवं अभ्यास का एक साधन है। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है? गायत्री मंत्र क्या देता है?
व्यक्तिगत विकास के कई तरीकों में से, मंत्र एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं में उपयोग किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंत्र प्रार्थना से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रार्थनाओं में सामान्य और समझने योग्य शब्दों का उपयोग किया जाता है, और मंत्रों में ध्वनियों, शब्दांशों और संयोजनों का उपयोग किया जाता है। जब सही ढंग से उच्चारण किया जाता है, तो एक अविश्वसनीय प्रभाव प्राप्त होता है। निर्धारित लक्ष्य अविश्वसनीय गति से हासिल किया जाता है।
गायत्री का अर्थ है आत्मा की मुक्ति और मंत्र का अर्थ है मानसिक शुद्धि। देवा प्रेमल गायत्री मंत्र का सुंदर प्रदर्शन करते हैं। उनका गायन एक उदाहरण है और कई अनुयायियों द्वारा दोहराया जाता है।
गायत्री मंत्र का अर्थ
यह मंत्र अन्य सभी मंत्रों में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। यह सभी बीमारियों और परेशानियों के लिए पेश किया जाता है। वह वेदों की पुस्तकों में प्रथम हैं। दूसरा भी कम शक्तिशाली मंत्र नहीं है साईं गायत्री। दोहराव के साथ अभ्यास सपनों को सच करने में मदद करता है।
प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करने से लाभ होता है:
- समस्त चेतना और मन को नकारात्मकता से शुद्ध करना;
- मौजूदा भ्रमों को दूर करता है;
- बुद्धि का स्तर विकसित करता है;
- उच्च योग्यताएँ प्रदान करता है;
- स्वास्थ्य बहाल करता है और सुंदरता बनाए रखता है;
- कल्याण और दीर्घायु सुनिश्चित करता है;
- अनिश्चितता, भय और असफलता को दूर करता है;
- आपको कठिनाइयों से उबरने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है।
चूँकि इसमें अत्यधिक शक्ति होती है, इसलिए इसका उपयोग बुरी नज़र और क्षति से मुक्ति के लिए किया जाता है।

पाठ और अनुवाद
अधिकांश मामलों में, निम्नलिखित प्रतिलेखन का उपयोग किया जाता है:
ॐ भूर् भुवः स्वाहा
तत् सवितुर वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्
मूल में यह इस तरह दिखता है
 लैटिन में इसे इस प्रकार लिखा जाता है
लैटिन में इसे इस प्रकार लिखा जाता है
(ओम भूर् भुवः स्वाहा
तत् सवितुर वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्)
रूसी में यह इस तरह दिखता है:

गायत्री मंत्र का अभ्यास कैसे करें
ऐसे कोई नियम नहीं हैं जिनका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता हो। सिफ़ारिशें हैं.
- सत्र या तो सूर्योदय के समय - सुबह, या सूर्यास्त के समय - शाम को किया जाना चाहिए। दोपहर के समय उच्चारित मंत्र लाभकारी प्रभाव डालता है।
- खाने से पहले मंत्र पढ़ने से शरीर शुद्ध और स्वस्थ रहेगा। और स्नान से पहले इसे कहने से आपका शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाएगी।
- आप इसे अपने लिए सुविधाजनक किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। साथ ही वह समय चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो।
- आपको मंत्र का पाठ 108 बार करना होगा। इस प्रयोजन के लिए समान संख्या में मनकों वाली मालाओं का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक पढ़ने के बाद, एक मनका घुमाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गिनती न छूटे।
- कोई भी और कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं कर सकती। सत्र मौन और एकांत में आयोजित किया जाता है। आप इन शब्दों को जितना अधिक दोहराएंगे, प्रभाव उतना ही बेहतर होगा।
- खाने या पानी की प्रक्रिया से पहले, तीन बार दोहराएं, नौ, ग्यारह।

मंत्र सत्र
किसी एकांत, शांत स्थान पर चले जाएँ। अपनी पीठ सीधी करके बैठें। मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आराम करना। छाती की दूरी पर सूर्य और देवी गायत्री के स्वरूप की कल्पना करें।
शब्दों का उच्चारण आपके लिए सबसे उपयुक्त तरीके से किया जाता है: फुसफुसाहट में, ज़ोर से, चुपचाप। मानसिक रूप से मात्रा का उच्चारण करने से सबसे अच्छा परिणाम मिलता है और इसमें शक्तिशाली शक्ति होती है। हालाँकि, यह विकल्प सबसे कठिन है। क्योंकि विचलित और भ्रमित होना बहुत आसान है। जब आप चिंतित हों और आपके विचार भटक रहे हों, तो इसे ज़ोर से करना बेहतर है।
पाठ का केवल उच्चारण ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और प्रेम भी डाला जाना चाहिए। तब आप जो कुछ भी करेंगे उसका अर्थ होगा। यदि आपकी अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है, तो शब्दों को पढ़ें और अपनी आवाज़ सुनें।
किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। यह ज्ञात है कि नकारात्मक विचार परेशानियों को आकर्षित करते हैं, और सकारात्मक विचार खुशी और प्यार को आकर्षित करते हैं। अच्छी चीजों के लिए खुद को तैयार करें! तब आपका जीवन बहुत अधिक रंगीन और दिलचस्प होगा।
वीडियो चयन
यह सभी वैदिक पवित्र सूत्रों का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी मंत्र है। गायत्री मंत्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो आत्मा और शरीर को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है, मनुष्यों के लिए इसका पवित्र अर्थ क्या है? आइए इसे लेख में देखें.
कर्म सफाई उपकरण
कर्म किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप होने वाली घटनाओं की एक क्रमिक श्रृंखला है। कोई भी असत्य, गलत तरीके से चुना गया मार्ग या किया गया कार्य भाग्य द्वारा भेजे गए परीक्षणों के रूप में व्यक्ति के पास वापस लौट आता है। कर्म के नकारात्मक प्रभाव से स्वयं को कैसे बचाएं? गायत्री मंत्र इसमें सहायता करता है।
हिंदुओं का मानना है कि गायत्री के दैनिक अभ्यास से व्यक्ति पुनर्जन्म की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। मनुष्य को पुनर्जन्म से मुक्ति क्या मिलती है? वेदों के अनुसार, वह स्वयं को सांसारिक दुनिया से अलग, एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है। मंत्र की शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि साधक के साथ-साथ उसके आस-पास की वस्तुएं और संपूर्ण स्थान भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए, हिंदू भोजन से पहले और पूजा से पहले गायत्री का जप करते हैं।
मंत्र के अभ्यास के दौरान, आप सीधे देवी गायत्री से संपर्क कर सकते हैं, जो ब्रह्मा की पत्नी हैं। पहले, केवल दीक्षित लोग ही गायत्री का अभ्यास कर सकते थे, लेकिन हाल ही में स्वर्ग ने इसे उन सभी को उपयोग करने की अनुमति दे दी है जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं।
मंत्र का उच्चारण वेदों की पवित्र भाषा संस्कृत में किया जाता है। यह अन्य भाषाओं में (अनुवाद में) नहीं किया जाता है: पवित्र ध्वनियों की लय खो जाती है। यह मंत्र ब्रह्मा के पुत्र विश्वामित्र द्वारा दीक्षार्थियों को प्रकट किया गया था। पवित्र पाठ सौर देवता - सूर्य को संदर्भित करता है, जो वेदों के दिव्य देवता पर हावी है।
गायत्री साधना
गायत्री वेदों की माता है जो जहां भी अपने मंत्र का अभ्यास किया जाता है वहां मौजूद रहती है। गायत्री के कंपन अभ्यासकर्ता के आध्यात्मिक शरीर को भर देते हैं, उसे बदलते हैं और उसे प्रबुद्ध करते हैं। गायत्री आध्यात्मिक मन को प्रबुद्ध और खोलती है, उसे भौतिक अंधकार से बाहर निकालती है और दिव्य सत्य और आनंद का सच्चा मार्ग दिखाती है। यह वह दिव्य शक्ति है जो अस्तित्व में मौजूद हर चीज़ को सांस देती है और पुनर्जीवित करती है। यह दैवीय शक्ति का अवतार है जो मनुष्य की रक्षा करता है।
गायत्री के तीन नाम हैं जो मानव आत्मा में विद्यमान हैं:
- भावनाएँ (गायत्री);
- महत्वपूर्ण ऊर्जा (सरस्वती);
- सच्चा ज्ञान (सावित्री)।
यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में विचारों (इरादों), वाणी और कार्यों में सामंजस्य बनाए रखता है, तो तीन दिव्य नाम उसमें निवास करते हैं - गायत्री, सरस्वती और सावित्री।
गायत्री मंत्र में तीन भाग हैं:
- देवता की पूजा;
- ध्यान;
- प्रार्थना अपील.
पवित्र पाठ के शुरुआती शब्द परमात्मा की पूजा का उल्लेख करते हैं। धीमहि शब्द का अर्थ है ध्यान की अवस्था। शेष 4 शब्द आध्यात्मिक क्षमताओं और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के अनुरोध के साथ ईश्वर से प्रार्थनापूर्ण अपील व्यक्त करते हैं।
मंत्र का निरंतर अभ्यास ठोस परिणाम लाता है:
- बीमारियों से छुटकारा;
- बुराई और परेशानियों से सुरक्षा;
- सपना सच हो गया;
- आध्यात्मिक मन का जागरण.
यदि आप विश्वास के साथ गायत्री का अभ्यास करते हैं, तो आप सभी आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको मंत्र का अभ्यास कब करना चाहिए? अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय संक्रमणकालीन समय माना जाता है - भोर, दोपहर, सूर्यास्त। ये घंटे आध्यात्मिक कार्यों और ध्यान के लिए सबसे अनुकूल माने जाते हैं। हालाँकि, आप किसी भी सुविधाजनक समय पर मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन निर्दिष्ट घंटों में आप अधिक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं।
गायत्री मंत्र के सही अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त हृदय और विचारों की शुद्धता है। गायत्री को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बोले गए प्रत्येक अक्षर की पवित्रता का अनुभव करना चाहिए। मंत्र का अभ्यास करने वाले को बुराई से बचना चाहिए, बुरे कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप बुरे शब्द नहीं बोल सकते, गाली नहीं दे सकते, या दूसरों को परेशान नहीं कर सकते। मन, वचन और कर्म हर चीज़ में पवित्रता के लिए प्रयास करना आवश्यक है।
योगी पानी से शुद्धिकरण के दौरान स्नान में मंत्र का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। जल की शक्ति, मंत्र की सफाई शक्ति के साथ, शरीर और विचारों को हर अशुद्धता से मुक्त कर देगी। मंत्र का अभ्यास सोने से पहले, जागने के बाद और खाने से पहले भी किया जा सकता है। अभ्यास पूरा करने के बाद आपको शांति शब्द को तीन बार बोलना चाहिए।
टिप्पणी! मंत्र के गलत अभ्यास से विपरीत परिणाम होगा!
अर्थ एवं अनुवाद
गायत्री मंत्र का पवित्र पाठ इस प्रकार है:
रूसी में सूत्र के कई अनुवाद हैं, वे सभी सही हैं। आइए किसी एक संस्करण के अनुवाद और अर्थ पर विचार करें:
- ओम सृष्टि का स्रोत है, परब्रह्म;
- भूर - भौतिक संसार;
- भुवः - मध्य जगत, सूक्ष्म तल;
- स्वाहा - स्वर्गीय दुनिया;
- तत् - ब्रह्म, ईश्वर;
- सवितुर - जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई;
- वरेण्यम - आदरणीय;
- भर्गो - दिव्य चमक;
- देवस्य - उच्चतम वास्तविकता (दिव्य);
- धीमहि - देवता का ध्यान;
- ध्यो - उच्चतम सत्य का एहसास कराना;
- यो - जो;
- नहीं - हमारा;
- प्रचोदयात् - सच्चे मार्ग पर चलने का निर्देश देता है।
गायत्री का प्रत्येक अक्षर मानव शरीर के एक विशिष्ट भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह शारीरिक बीमारियों से पूरी तरह से शुद्ध करता है:
रूसी में साहित्यिक अनुवाद में, मंत्र का पाठ इस तरह लगता है:
किसी मंत्र का सही उच्चारण करने के लिए, आपको पहले किसी रिकॉर्डिंग को सुनना होगा, उदाहरण के लिए, प्रदर्शन किया गया। इस समर्पित यूरोपीय महिला का प्रेरित प्रदर्शन आत्मा को स्वर्ग से आने वाले आनंद से भर देता है। सबसे पहले, आप बस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि ध्वनियाँ आपके शरीर और आत्मा को कैसे छूती हैं। फिर आप प्रत्येक पवित्र शब्द के प्रति सचेत रहते हुए गायक के साथ दोहरा सकते हैं।
मंत्र का जाप अर्ध कमल की स्थिति में, सीधी रीढ़ की हड्डी के साथ करना बेहतर होता है। आप झुककर बैठ या खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि रीढ़ से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो अंतरिक्ष से सिर के शीर्ष से होकर आती है। हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें, क्योंकि यह जीवन की जड़ है। सीधी पीठ शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की कुंजी है।
अभ्यास के पहले समय में अकेले रहने का प्रयास करें ताकि कोई आपको परेशान न करे। दूसरों की आलोचनात्मक टिप्पणियाँ या उनकी जिज्ञासा अभ्यास के परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। आप हेडफ़ोन लगाकर सुन सकते हैं और शब्दों को अपने आप दोहरा सकते हैं। हालाँकि, इसे ज़ोर से कहने से अधिक प्रभाव पड़ेगा - शरीर में कंपन इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। इस मामले में, भौतिक शरीर दैवीय ऊर्जा का प्राप्तकर्ता बन जाता है।
मन में बार-बार दोहराने से भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर आपको उपचार की जरूरत है तो मंत्र का जाप जोर से करें। आप एक अलग अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं: हेडफ़ोन में रिकॉर्डिंग सुनें और कल्पना करें कि कैसे पवित्र ध्वनियाँ शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवेश करती हैं और उसे ठीक करती हैं, बीमारी से मुक्त करती हैं। ध्यान के दौरान बाधित न होने के लिए कहें।
गायत्री मंत्र सबसे लोकप्रिय मंत्रों में से एक है। हिंदू इसे आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के तरीकों में से एक मानते हैं। वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन मंत्रों का जाप किया जाता है। माना जाता है कि शब्दों के क्रम और उनकी ध्वनि के कारण गायत्री मंत्र विशेष शक्ति से संपन्न है।
लेख में:
गायत्री मंत्र - यह क्या है?
गायत्री मंत्र उन मंत्रों में से एक है जिसे अक्सर दुनिया भर के लोगों द्वारा दैनिक अभ्यास में उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार व्यक्ति सूर्य की ऊर्जा की ओर मुड़ता है। मंत्र रिकार्ड किया गया वेदों, और ऋषि को धन्यवाद देते हुए प्रकट हुए विश्वामित्र, सबसे सम्मानित नायकों में से एक वेद, ईश्वर का पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मांड के पूर्वज.
गायत्री मंत्र एक सार्वभौमिक प्रार्थना है, जिसे मनुष्य के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ वेदों में सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है।
"सत्य साईं बोलते हैं"
 हिंदुओं का मानना है कि मंत्र अपनी शक्ति में सामान्य प्रार्थनाओं से भिन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र अनावश्यक विचारों से छुटकारा पाने में मदद करता है, मन को शुद्ध करता है और अस्तित्व के उच्चतम अर्थ की ओर इशारा करता है। कुछ सूत्रों का कहना है कि मंत्र का दैनिक जाप बुरी नज़र से बचाता है, कर्म को रद्द करता है और यहां तक कि कई विश्व धर्मों के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है - चक्र से बाहर निकलना संसार, शाश्वत पुनर्जन्म का चक्र, दूसरी दुनिया में जाना, लेकिन पिछले जन्मों को स्मृति में और चेतना खोए बिना बनाए रखना।
हिंदुओं का मानना है कि मंत्र अपनी शक्ति में सामान्य प्रार्थनाओं से भिन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र अनावश्यक विचारों से छुटकारा पाने में मदद करता है, मन को शुद्ध करता है और अस्तित्व के उच्चतम अर्थ की ओर इशारा करता है। कुछ सूत्रों का कहना है कि मंत्र का दैनिक जाप बुरी नज़र से बचाता है, कर्म को रद्द करता है और यहां तक कि कई विश्व धर्मों के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है - चक्र से बाहर निकलना संसार, शाश्वत पुनर्जन्म का चक्र, दूसरी दुनिया में जाना, लेकिन पिछले जन्मों को स्मृति में और चेतना खोए बिना बनाए रखना।

कई आध्यात्मिक आंदोलन गायत्री को अन्य मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मानते हैं।
अधिक सांसारिक प्रथाओं में, खाने से पहले पाठ गाया जाता है, जिससे भोजन साफ हो जाता है, पानी की प्रक्रिया लेने से पहले, आंतरिक स्थान साफ हो जाता है। मंत्र को तीन, नौ या ग्यारह बार पढ़ा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि जप करते समय साधक देवी को संबोधित करता है गायत्री. यह देवी के नामों में से एक है सावित्री, भगवान की पत्नी ब्रह्माऔर चारों वेदों की माता. मध्य युग में, ब्राह्मणों के दैनिक अभ्यास के लिए पाठ का जप अनिवार्य माना जाता था। अन्य जातियों को मंत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालाँकि, बाद में यह गाना सभी जातियों, महिलाओं के लिए उपलब्ध हो गया। आजकल, मंत्र दुनिया भर में गाया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।
गायत्री मंत्र के पाठ में तीन पारंपरिक भाग होते हैं: रूपांतरण, ध्यान और प्रार्थना। . हिंदू धर्म के सभी मंत्रों की तरह, पाठ संस्कृत में गाया जाता है। निम्नलिखित नुसार:
संस्कृत में:
ॐ भूर्भुवः स्वः ।
तत् सवितुर्वरेण्यं ।
भर्गो देवस्य धीमहि ।
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥
लैटिन में:
ॐ भूर् भुवः स्वाहा
तत् सवितुर वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्
रूसी में:
ॐ भूर् भुवः स्वाहा
तत् सवितुर वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्
संस्कृत की विशिष्टताओं के कारण, जिसमें हिंदू धर्म के सभी पवित्र ग्रंथ लिखे गए थे, मंत्र के अनुवाद बड़ी संख्या में हैं। यहां कुछ सर्वाधिक लोकप्रिय हैं।
प्रत्येक शब्द के अलग-अलग अर्थ का शब्द-दर-शब्द अनुवाद इस प्रकार है:
- पवित्र शब्दांश ॐ, मतलब सातवां चक्र सहस्रार, मुख्य पाठ को प्रारंभ और समाप्त करता है। समस्त ज्ञान का प्रतीक है।
- भूर, भुव, सुवहावे तीन प्रकार की सृष्टि की बात करते हैं: भौतिक, सूक्ष्म और स्वर्गीय।
- गूंथनाउस सर्वोच्च देवता का प्रतीक है जिससे अपील की जाती है।
- सवितुरमतलब सर्वशक्तिमान.
- भरगो- उच्चतम शुद्ध प्रकाश।
- जाम देवस्य- दिव्य वास्तविकता.
- धिमाही- हम ध्यान करते हैं या उच्च शक्तियों से संपर्क करते हैं।
- धियो- बुद्धिमत्ता।
- यो- कौन सा।
- नः- हमारा।
- प्रचोदयात्- प्रबुद्ध करेगा.
साहित्यिक अनुवाद:
“हे सर्वशक्तिमान, ब्रह्मांड के निर्माता, जीवन के दाता, दर्द और पीड़ा को दूर करने वाले और खुशी के दाता! आप पापों का नाश करने वाली सर्वोच्च ज्योति हैं। हम आपका ध्यान करते हैं ताकि आप हमारे मन को प्रेरित करें, प्रबुद्ध करें और सही दिशा में ले जाएं!
धन्वंतरि- अवतार विष्णु, जिसकी बदौलत लोगों को इसके बारे में पता चला आयुर्वेद. कई सहस्राब्दियों से, कई अनुष्ठान और प्रार्थनाएँ की गईं धन्वंतरि. मूल मंत्र अपील:
ॐ नमो भगवते धन्वन्तराय स्वाहा
इस प्रकार अनुवादित: “ओम. दिव्य धन्वंतरि को श्रद्धांजलि". अधिकतर डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पाठ की मदद से एक व्यक्ति दूसरे की बीमारियों को अधिक सूक्ष्म स्तर पर देख पाता है। पवित्र पाठ किसी भी औषधि की शक्ति को बढ़ाता है, विशेषकर पौधों के आधार पर बनी औषधियों की। आयुर्वेद में, यह माना जाता है कि सादे पानी पर इक्कीस बार मंत्र का जाप करने के बाद, तरल उपचार अमृत में बदल जाता है।

अन्य स्रोतों का कहना है कि जो लोग प्रतिदिन एक सौ आठ बार मंत्र का अभ्यास करते हैं वे अपने हाथ के स्पर्श से ठीक हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रार्थना करने से व्यक्ति को बुरी नज़र और बीमारियों से शक्तिशाली सुरक्षा मिलती है।
रूसी में मंत्र का पूरा पाठ इस प्रकार है:
ओम् शंखम चक्रम जलौकम
दधाद अमृत घटं चारु डोर्बिश चतुर्भिः
सूक्ष्म स्वच्छहृदयमशुका परिविलासन मौलिक अम्भोजा नेत्रम्
कालम्भोदज्ज्वलंगम् कटि तत् विलासच चारु पीताम्बरद्यम्
वन्दे धन्वन्तरिम् तम निखिल गदा वन प्रौधा दावाग्नि लीलम्
साहित्यिक अनुवाद:
“धन्वंतरि को नमस्कार, जिनके चार हाथों में शंख, चक्र, जोंक और अमृत का पात्र है; जिसके हृदय में सूक्ष्मतम, शुद्धतम, आनंदमय प्रकाश चमकता है। यह प्रकाश उनके सिर के चारों ओर, उनकी कमल आंखों के आसपास भी चमकता है; जो अपनी एक लीला से समस्त रोगों को जंगल की भीषण अग्नि के समान नष्ट कर देता है।”
 मंत्रों का जाप सूर्योदय, दोपहर या सूर्यास्त के समय करने की सलाह दी जाती है। गंभीर अभ्यासी बिना किसी रुकावट या ध्यान भटकाए पवित्र पाठ का एक सौ आठ बार जाप करते हैं। गिनती खोने से बचने के लिए माला के मोतियों का प्रयोग किया जाता है। मंत्र को जितनी अधिक बार गाया जाता है, प्रभाव उतना ही अधिक होता है। पाठ का सही क्रम में उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण है।
मंत्रों का जाप सूर्योदय, दोपहर या सूर्यास्त के समय करने की सलाह दी जाती है। गंभीर अभ्यासी बिना किसी रुकावट या ध्यान भटकाए पवित्र पाठ का एक सौ आठ बार जाप करते हैं। गिनती खोने से बचने के लिए माला के मोतियों का प्रयोग किया जाता है। मंत्र को जितनी अधिक बार गाया जाता है, प्रभाव उतना ही अधिक होता है। पाठ का सही क्रम में उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण है।

अभ्यास के लिए किसी शांत जगह का चुनाव करें, आपको उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होना है, अपनी पीठ सीधी रखें। वे एक रिकॉर्डिंग के लिए, उन्नत चरण में - अपने आप, जोर से या फुसफुसाहट में गाते हैं, और केवल सबसे प्रबुद्ध लोग ही अपने होंठ खोले बिना मंत्र का जाप कर सकते हैं। उत्तरार्द्ध विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि आने वाले विचार एकाग्रता की अनुमति नहीं देते हैं और अभ्यासकर्ता को लगातार भ्रमित करते हैं।
गायन के क्रम में व्यक्ति देवी की छवि की कल्पना करता है गायत्रीया स्वयं, दूसरों, दुनिया के प्रति कृतज्ञता की भावना पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है।
बी. ए. ज़ागोरुल्को
यह कार्य (सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं में) दो प्रसिद्ध मंत्रों - "गायत्री" और "साईं गायत्री" की जांच करता है।
इनमें से पहला, गायत्री मंत्र, वेदों का सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि इसमें उनका संपूर्ण सार समाहित है। इस मंत्र का जाप सभी धर्मनिष्ठ हिंदुओं के दैनिक अनुष्ठान का हिस्सा है। यह मंत्र, जो सीधे हमारे ब्रह्मांड के ईश्वर (ईश्वर) को संबोधित है, जिसे सवितार कहा जाता है, एक व्यक्ति को ईश्वर की चेतना के साथ एकता की ओर ले जा सकता है और इस प्रकार देवी गायत्री द्वारा व्यक्त उसकी शक्ति के माध्यम से उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
दूसरा - साईं गायत्री मंत्र - हमारी सदी के अवतार (मानव रूप में भगवान) का मंत्र है - श्री सत्य साईं बाबा, जिन्हें शिव (ब्रह्मांडीय चेतना) और शक्ति (ब्रह्मांडीय ऊर्जा) का एक साथ अवतार माना जाता है। अवतार की दिव्य कृपा के माध्यम से इस मंत्र का अभ्यास व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति से लेकर परम मुक्ति (मोक्ष) तक सब कुछ प्रदान कर सकता है।
पहला अध्याय मंत्र योग के कुछ मूलभूत मुद्दों (मंत्र का सार, इसकी क्रिया का सिद्धांत, जप के अभ्यास में स्तर, आदि) पर चर्चा करता है। कार्य का मूल्य इस तथ्य में भी निहित है कि पहली बार रूसी में (सरलीकृत रूप में, अक्षरों को लंबवत रूप से स्थानांतरित करके) मंत्र की एक इंटोनेशन रिकॉर्डिंग दी गई है, जिससे इसे पुन: पेश करना आसान हो गया है। यह कार्य धर्मों के इतिहास, हिंदू धर्म और योग के सिद्धांत और अभ्यास में रुचि रखने वाले पाठकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए है।
बी.ए. ज़ागोरुल्को, एन.एन. सैमसोनोवा: "साई वेद", 1997।
मंत्र और जप
प्राचीन भारतीय ऋषियों के दर्शन के अनुसार, हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड सर्वोच्च वास्तविकता की एक बाहरी अभिव्यक्ति है, जो बुद्धि के माध्यम से ज्ञान के लिए अप्राप्य है। यह पारलौकिक वास्तविकता या, हिंदू शब्दावली में, ब्रह्म एक ओर स्वयं को निर्जीव ब्रह्मांड के रूप में प्रकट करता है, और दूसरी ओर चेतना या आत्माओं के अनगिनत केंद्रों के रूप में प्रकट होता है। ये आत्माएं खुद को पहले इन्वोल्यूशन (पदार्थ में उतरना), और फिर विकास (आत्मा की ओर चढ़ना) की एक लंबी प्रक्रिया में शामिल पाती हैं, जो कई अवतारों तक फैली हुई है और संसार के तथाकथित चक्र (जन्म और मृत्यु का चक्र) का प्रतिनिधित्व करती है। आत्माओं के विकास का अंतिम लक्ष्य उनकी दिव्यता के बारे में जागरूकता और संसार के चक्र से बाहर निकलना, यानी मोक्ष (अंतिम मुक्ति) की उपलब्धि है। आत्माएं विकास और विकास की प्रक्रियाओं में क्यों शामिल थीं, यह एक विशेष प्रश्न (अतिप्रश्न) है, जिसका उत्तर बुद्धि के स्तर पर नहीं दिया जा सकता है और जिसे केवल आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद ही हल किया जा सकता है।
बिना किसी अपवाद के, इस संसार में सभी जीवित प्राणी सुख के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन कितने लोग इसे हासिल कर पाते हैं? मानव बुद्धि की अत्यधिक प्रगति के बावजूद, दर्द, पीड़ा और मृत्यु दुनिया में हर जगह देखी जा सकती है। और फिर भी पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग हैं और हमेशा रहे हैं, जिन्होंने सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, निरंतर आनंद में हैं और मानवता को इसे प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। यह वे हैं - ऋषि और योगी - जो हमें बताते हैं कि खुशी का स्रोत केवल अपने भीतर ही पाया जा सकता है, अपनी चेतना को उच्च, दिव्य स्तर तक बढ़ाकर, निचले जीवन के भ्रमों और सीमाओं पर काबू पाकर। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक सुधार का मार्ग अपनाना होगा।
साधना के एक उपकरण के रूप में मंत्र
ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाने वाले कई प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास या मार्ग हैं: अनुष्ठान पूजा, प्रार्थना, ध्यान, योग के विभिन्न रूप आदि। संस्कृत में, आध्यात्मिक अभ्यास को साधना कहा जाता है, और इसमें लगे व्यक्ति को साधक कहा जाता है आध्यात्मिक अभ्यास में लगा हुआ व्यक्ति है, यानी, साधना का अभ्यासी [कम सामान्यतः - साधक: महिला लिंग - साधिका])। साधना व्यक्तिगत प्रयास (मूल "साध" का अर्थ है "प्रयास करना") के माध्यम से चेतना के उच्च और उच्चतर स्तरों के क्रमिक और प्रगतिशील रहस्योद्घाटन का एक लंबा मार्ग है जब तक कि मानव विकास का अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता - भगवान के साथ एकता। किसी भी साधना का मूल सिद्धांत व्यक्ति में सत्व गुण (किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक सिद्धांत से जुड़े प्रकृति के मौलिक गुणों में से एक) को बढ़ाना है। भारत में साधना के सबसे सामान्य रूपों में से एक (विशेषकर इसके प्रारंभिक चरण में) मंत्र या जप का दोहराव है।
साधना के एक साधन के रूप में मंत्र वैदिक काल से जाना जाता है और यह एक विशेष रूप से भारतीय घटना है। स्वयं वेद, जिन्हें ईश्वर का रहस्योद्घाटन माना जाता है, मंत्रों से युक्त पवित्र ग्रंथों के संग्रह से अधिक कुछ नहीं हैं।
संसार के सभी धर्मग्रन्थ इस बात पर एकमत हैं कि हमारा संसार शब्द की सहायता से बना है। बाइबल के रूसी अनुवाद में हम पढ़ते हैं, "आरंभ में वचन था"। मूल ग्रीक में ऐसा लगता है जैसे "शुरुआत में लोगो था।" वेद कहते हैं: “प्रजापतिर वै इदं असित। तस्य वाग् द्वितीय असित" - "वास्तव में केवल प्रजापति (भगवान) ही अस्तित्व में थे। उसके साथ दूसरा था वक् (वाणी, वचन)।”
शास्त्रों के अनुसार, सर्वोच्च वास्तविकता की प्राथमिक अभिव्यक्ति शब्द नामक मौलिक कंपन के माध्यम से होती है, जिसका अर्थ ध्वनि या शब्द है। शब्द या ध्वनि रूप में ब्रह्म को शब्दब्रह्म कहा जाता है। इस अर्थ में यह ग्रीक लोगो से मेल खाता है, जिसका अर्थ शब्द और विचार दोनों है। शब्द अपने सूक्ष्म रूप में विचार है। रचनात्मक शक्ति के पहलू में यह शब्द-विचार एक पवित्र भाषण या मंत्र है।
सामान्य भाषाई उच्चारण के विपरीत, एक मंत्र, जिसमें सामान्य भाषा की तरह, वाक्य, शब्द, शब्दांश या ध्वनियाँ भी शामिल हो सकती हैं, में एक निश्चित रहस्यमय शक्ति होती है। यह इस शक्ति के माध्यम से है, पवित्र बीज मंत्र (शाब्दिक रूप से "मंत्र-बीज", अर्थात, वह मंत्र जिससे अन्य मंत्र विकसित होते हैं। ऐसे मंत्र वस्तुओं और वास्तविकता की घटनाओं के प्रोटोटाइप के रूप में कार्य करते हैं।) ओम का निर्माण और रखरखाव हमारे द्वारा किया जाता है ब्रह्मांड। यहां से साधना के उपकरण के रूप में मंत्र की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। यदि कोई मंत्र ईश्वर की शक्ति है, तो इस शक्ति की "निपुणता" ईश्वर की समझ की ओर ले जाती है।
मंत्र का आध्यात्मिक उद्देश्य
परिभाषा के अनुसार, मंत्र ध्वनियों का एक संयोजन है जिसमें एक निश्चित शक्ति होती है, जो सही ढंग से उच्चारण करने पर विशेष परिणाम देने में सक्षम होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ध्वनि पक्ष यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मंत्र के ध्वनि गुण हैं, जिनमें एक निश्चित ऊर्जा होती है, जो मंत्र को प्रार्थना से अलग करती है।
प्रार्थना और मंत्र के बीच मुख्य अंतर यह है कि प्रार्थना में मुख्य बात इसका अर्थ है, और इसलिए इसे किसी भी शब्द में व्यक्त किया जा सकता है, और किसी भी भाषा में अनुवाद भी किया जा सकता है। इसका प्रभाव पूरी तरह से इसमें डाली गई विचार की शक्ति पर निर्भर करता है, न कि इसकी ध्वनि विशेषताओं पर। गलत उच्चारण करने पर, मंत्र की शक्ति जागृत न होने पर मंत्र सामान्य प्रार्थना की तरह ही कार्य करता है।
प्रत्येक मंत्र का अपना देवता, अपना मीट्रिक आकार, ऋषि (द्रष्टा जिसने दुनिया को यह मंत्र दिया), शक्ति (शक्ति या ऊर्जा), कार्य का एक निश्चित क्षेत्र और एक विशिष्ट व्यावहारिक उद्देश्य होता है। मंत्र कई अन्य विशेषताओं में भी एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं: व्यक्तिपरक उद्देश्यों में, प्रभाव की ताकत और गति में, भाषाई संरचना में, आदि। मंत्रों के सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरणों में से एक पूजा की वस्तु के आधार पर उनका विभाजन है।
ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मंत्र के पीछे एक विशिष्ट देवता - देवता होता है। देवता एक सर्वोच्च ईश्वर के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं - उनके किसी भी कार्य या शक्ति का। सभी देवताओं में चेतना और शक्ति होती है, हालाँकि, जिनमें इनमें से एक पहलू अधिक हद तक प्रकट होता है, उन्हें क्रमशः उनके पुरुष और महिला रूपों में दर्शाया जाता है और देव (देवता) या देवी (देवी) कहा जाता है। उनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट नाम और एक विशिष्ट (आमतौर पर मानवरूपी) छवि या रूप से मेल खाता है जिसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। इसलिए विभिन्न देवताओं को समर्पित मंत्र: शिव (ओम नमः शिवाय), गणेश (ओम श्री गणेशाय नमः), काली (ह्रीं श्रीं क्रीं आद्या कालिका परमेश्वरी स्वाहा), राम (श्री राम जया राम जया जया राम), आदि।
उनके प्रभाव की प्रकृति के अनुसार, सभी मंत्रों को दो बड़े वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: मंत्र जिनका जादुई प्रभाव होता है (प्रकृति में परिवर्तन का कारण बनता है), और मंत्र जिनका आध्यात्मिक प्रभाव होता है (चेतना में परिवर्तन का कारण बनता है)। पहले लगभग मंत्र, मंत्र, ताबीज आदि के बराबर हैं, और प्राचीन काल से सभी लोगों द्वारा उपयोग किए जाते रहे हैं और सभी भाषाओं में मौजूद हैं। दूसरा - विशेष रूप से भारतीय प्रकार - आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अभिप्रेत है।
ध्वनि कंपन की कुछ और विशेषताएँ बताना भी आवश्यक है। ऊर्जा के मौलिक रूपों में से एक होने के नाते, ध्वनि चेतना से जुड़ी है और दिव्य चेतना का एक उपकरण है। ध्वनि कंपन न केवल किसी भी रूप के आधार पर निहित है, बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति के लिए भी नितांत आवश्यक है। इस कारण ध्वनि ही चेतना को सीधे प्रभावित करने में सक्षम है। अनुभूति की प्रक्रिया में इसका एक कार्य चेतना की अवस्थाओं को बदलना है। आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए मंत्र का उपयोग, किसी व्यक्ति की चेतना की अवस्थाओं को बदलकर उसकी उच्चतम प्रकृति को प्रकट करने के साधन के रूप में, मंत्र योग नामक एक विशेष अनुशासन का गठन करता है। प्रत्येक प्रकार की साधना का अपना उद्देश्य होता है। मंत्र योग का लक्ष्य साधक की चेतना की चुने हुए देवता (इष्ट-देवता) की चेतना के साथ पूर्ण एकता प्राप्त करना है। सामान्य मानव चेतना और उच्चतर, दिव्य चेतना के बीच की बाधा को खत्म करने की मंत्र की क्षमता मंत्र योग का आधार है।
किसी मंत्र को प्रभावी बनाने के लिए, ध्वनि संयोजनों (मंत्र-शक्ति) में छिपी शक्ति को साधना (साधना-शक्ति) की प्रक्रिया में साधक के प्रयासों के माध्यम से जागृत किया जाना चाहिए। मंत्र की क्रिया मंत्र-शक्ति और साधना-शक्ति के संयोजन से होती है। इस मामले में, तथाकथित मंत्र-चैतन्य उत्पन्न होता है (शाब्दिक रूप से, "मंत्र की चेतना"), जो मंत्र को नियंत्रित करने वाले देवता की चेतना के साथ साधक की चेतना के मिलन की ओर ले जाता है। साधक चेतना और देवता चेतना का एकीकरण ही चेतना का जागरण या उद्घाटन है, जो मंत्र योग का लक्ष्य है।
यदि गैर-आध्यात्मिक उद्देश्य वाले मंत्रों का उपयोग करते समय, उनका प्रभाव अक्सर बहुत जल्दी और कभी-कभी तुरंत प्रकट हो सकता है, तो विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक उद्देश्य वाले मंत्रों को दीर्घकालिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि साधक की चेतना को शुद्ध किया जाना चाहिए और इसके लिए तैयार किया जाना चाहिए। रहस्योद्घाटन. इसे तुरंत रूपांतरित नहीं किया जा सकता. मंत्र का उद्देश्य जितना ऊँचा होगा, उसके निष्पादन की तकनीक उतनी ही सरल और सुरक्षित होगी और तदनुसार, पूर्ण परिणाम प्राप्त करने में उतना ही अधिक समय लगेगा।
किसी मंत्र का तीव्र और अधिक ध्यान देने योग्य प्रभाव डालने के लिए, सबसे पहले, उसका अर्थ जानना, उसका सही उच्चारण करने में सक्षम होना आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से प्राप्त किया जाना चाहिए, जो कि है एक सच्चा गुरु (आध्यात्मिक शिक्षक) होना चाहिए। इस मामले में, मंत्र को पहले से ही "जागृत" माना जाता है और इसमें ऊर्जावान शक्ति होती है। यह सच है। हालाँकि, पर्याप्त प्रयास, उच्च एकाग्रता और पूजा की वस्तु के प्रति समर्पण के साथ, मंत्र की शक्ति (मंत्र-शक्ति) स्वयं को "जागृत" कर सकती है। मंत्र का जागरण उसके बार-बार दोहराए जाने, स्पष्ट और सही उच्चारण, उचित स्वर और लय को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
जाप
जप चेतना की उच्च अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से एक मंत्र का दोहराव है। किसी मंत्र को दोहराने से विभिन्न स्तरों पर कुछ कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन, बदले में, साधक के विभिन्न शरीरों को प्रभावित करते हैं और उनमें परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उनके पदार्थ को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, चेतना के विभिन्न वाहनों को इस तरह से शुद्ध और सुसंगत किया जाता है कि चेतना की उच्च अवस्थाओं की अभिव्यक्ति संभव हो जाती है।
मंत्र को जोर से, फुसफुसाकर या चुपचाप दोहराया जा सकता है। जब ज़ोर से दोहराया जाता है, तो भौतिक ध्वनियाँ भौतिक शरीर को प्रभावित करती हैं। फुसफुसाहट में दोहराए जाने पर मंत्र साधक के सूक्ष्म (ईथर) शरीर पर कार्य करता है और उसमें परिवर्तन उत्पन्न करता है। मानसिक रूप से दोहराने पर मंत्र उसके मन पर तदनुसार प्रभाव डालता है। मानसिक जप सबसे प्रभावशाली माना जाता है।
किसी मंत्र के मानसिक दोहराव के कई चरण होते हैं। पहले चरण में, मन स्वयं ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करता है और केवल उनके प्रति जागरूक होता है। दूसरे चरण में शब्दों की ध्वनि के साथ-साथ उनके अर्थ का स्वतः ही बोध हो जाता है। तीसरे चरण में अलग-अलग शब्दों के अर्थ के स्थान पर संपूर्ण मंत्र का अर्थ बोध होता है। लंबे अभ्यास और एकाग्रता से पूरे मंत्र का सामान्य विचार अधिक से अधिक स्थिर हो जाता है और लगभग लगातार दिमाग में मौजूद रहता है। इस स्तर पर, हालांकि मंत्र का मानसिक रूप से उच्चारण जारी रहता है, शब्द पृष्ठभूमि में फीके पड़ जाते हैं और (भारतीय संगीत वाद्ययंत्र - तानपुर की तरह) बस मुख्य विचार के लिए एक सामान्य पृष्ठभूमि बनाते हैं, जो लगातार दिमाग में मौजूद रहता है। यह वह स्तर है जिस तक एक सामान्य साधक पहुँच सकता है।
हालाँकि, यदि जप करने वाला मन से परे की वास्तविकता को समझना चाहता है, तो उसे अभ्यास के चौथे चरण पर चढ़कर मन के स्तर को पार करना होगा, जो वास्तव में समाधि (ट्रान्स अवस्था) के चरण को चिह्नित करता है। यह पूजा की वस्तु के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस स्थिति में, साधक को स्वयं के बारे में पता होना बंद हो जाता है, और उसकी चेतना पूरी तरह से मन में मौजूद विचार के साथ विलीन हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है।
इस अवस्था तक पहुँचने के लिए साधक को अपनी भावनात्मक प्रकृति, मानसिक एकाग्रता और इच्छाशक्ति का उपयोग करके अपनी सभी शक्तियों को संयोजित करना होगा। जप का अभ्यास अधिक प्रभावी हो जाता है यदि इसके साथ चुने हुए देवता का दर्शन भी हो। सिद्धांत रूप में, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि छवि कहाँ और कैसे बनाई जाए, क्योंकि यह अभी भी दिमाग में बनती है। इसके लिए उपयुक्त स्थान आध्यात्मिक हृदय माना जाता है, जो प्रतीकात्मक रूप से छाती के केंद्र में स्थित है। अपने मन में देवता की छवि स्वयं बनाना जरूरी है। श्री सत्य साईं बाबा कहते हैं, "जब मन भगवान का रूप बनाता है, तो वह स्वयं वह रूप बन जाता है, और भगवान स्वयं उस रूप को अपनी दिव्यता से भर देते हैं।"
गायत्री मंत्र
मन को शुद्ध किए बिना और किसी व्यक्ति में बुद्धि के सिद्धांत को विकसित किए बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है, जिसका मुख्य कार्य सत्य और असत्य के बीच अंतर करना है। बुद्धि बुद्धि की तुलना में उच्च स्तर की क्षमता है, जिसे यूरोपीय शब्दावली में अंतर्ज्ञान (शाब्दिक रूप से "प्रत्यक्ष अनुभूति") कहा जाता है। बौद्धिक ज्ञान को सच्चा ज्ञान बनने के लिए, इसे बुद्धि के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। विकास या, अधिक सटीक रूप से, स्वयं के भीतर बुद्धि की खोज सचेतन आध्यात्मिक अभ्यास का प्रारंभिक बिंदु है। हिंदू धर्म में यह भूमिका गायत्री मंत्र द्वारा निभाई जाती है। इस मंत्र का पाठ इस प्रकार है:
ॐ भूर् भुवः स्वाहा
तत् सवितुर वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्
ॐ! सांसारिक, सूक्ष्म और स्वर्गीय संसारों को आशीर्वाद! आइए हम सवितार (ईश्वर की दिव्य महिमा का प्रतीक) के उज्ज्वल प्रकाश पर ध्यान करें! क्या वह हमारे मन को प्रकाशित कर सकता है!
गायत्री* शब्द का प्रयोग हिंदू धर्मग्रंथों में तीन अलग-अलग अर्थों में किया जाता है। सबसे पहले, यह शब्द एक प्रसिद्ध मंत्र को संदर्भित करता है, जिसका दोहराव सभी धर्मनिष्ठ हिंदुओं के दैनिक धार्मिक अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा वह काव्य छंद है जिसमें यह मंत्र लिखा गया है, और तीसरा वह देवी है जो इस मंत्र की शक्ति को व्यक्त करती है।
(*गायत्री" - यह बिल्कुल वही तनाव है (अर्थात अंतिम अक्षर पर) जो दुनिया के सबसे आधिकारिक और प्रसिद्ध संस्कृतज्ञों में से एक, मोनियर-विलियम्स, अपने "संस्कृत-अंग्रेजी" शब्दकोश में देते हैं।)
गायत्री मंत्र का उद्देश्य
शब्द "गायत्री" (अंतिम अक्षर पर स्त्रीलिंग उच्चारण के साथ) का शाब्दिक अर्थ है "जिसके जप से मोक्ष प्राप्त होता है" (जहाँ "गा" - "जप करना", "त्रि" - "बचाना")। शब्द "गायत्र" (पुरुष और मध्यम वर्ग) का एक और संस्करण, जैसा कि साईं बाबा बताते हैं, व्युत्पत्ति के अनुसार "वह जो व्यक्तिगत आत्माओं की रक्षा करता है" (जहां "गया" का अर्थ है "व्यक्तिगत आत्माएं - जीव", "त्र" का अर्थ है " रक्षा करना "). इस प्रकार, शब्द का अर्थ ही आध्यात्मिक अभ्यास के उच्चतम लक्ष्य - मोक्ष या मुक्ति, साथ ही मंत्र की उच्चतम शक्ति को इंगित करता है, जो इसका अभ्यास करने वाले की रक्षा कर सकता है।
गायत्री मंत्र का मुख्य उद्देश्य, जिसमें साधक भगवान को "वह हमारे मन को प्रकाशित करें!" शब्दों के साथ सर्वोच्च चेतना के उज्ज्वल प्रकाश के रूप में संबोधित करता है, जहां "मन" शब्द का अर्थ "बुद्धि" है, ठीक इसी को प्रकट करना है किसी व्यक्ति के सिद्धांत में सर्वोच्च। यह भी महत्वपूर्ण है कि गायत्री मंत्र का अभ्यास चेतना का क्रमिक और प्रगतिशील उद्घाटन सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने गायत्री मंत्र को हिंदुओं के दैनिक धार्मिक अभ्यास का अनिवार्य हिस्सा बना दिया।
अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करते हुए आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति का प्राथमिक कार्य मुक्ति प्राप्त करना नहीं है (क्योंकि यह एक जीवन का काम नहीं है), बल्कि अपनी अज्ञानता को खत्म करना है, जिसमें एक भ्रामक दृष्टि शामिल है दुनिया के। इसके लिए चेतना के सभी निचले वाहनों की शुद्धि और पुनर्गठन की आवश्यकता होती है, ताकि सत्य के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति के पास उच्च आध्यात्मिक स्तरों पर काम करने के लिए अधिक सूक्ष्म उपकरण हो सकें। यह बुद्धि का प्रकाश है, जिसका जागरण गायत्री मंत्र के अभ्यास से होता है। यदि कोई व्यक्ति, लगातार गायत्री जप का अभ्यास करता है, ईमानदारी से उस प्रकाश के लिए प्रयास करता है, जो केवल भीतर से, उसकी आभा में आ सकता है, जैसा कि गायत्री मंत्र के सबसे गहन शोधकर्ताओं में से एक प्रोफेसर आई.के. तैम्नी लिखते हैं (आई.के. तैम्नी देखें। गायत्री: दैनिक हिंदुओं की धार्मिक प्रथा। अडयार: मद्रास, 1974.), एक विशेष तनाव पैदा होता है, जो उच्च स्तर की दिव्य शक्ति की उसकी चेतना में उतरने के लिए एक चैनल खोलता है।
ईश्वर का ज्ञान तीन स्तरों पर किया जा सकता है: मन (मानस) या बुद्धि के स्तर पर; अंतर्ज्ञान (बुद्धि) या आध्यात्मिक धारणा के स्तर पर और वास्तविकता के स्तर पर, सीधे - ईश्वर की चेतना के साथ अपने उच्च स्व (आत्मा) के विलय के माध्यम से। गायत्री मंत्र इन तीनों स्तरों पर ऐसा ज्ञान देने में सक्षम है।
गायत्री मंत्र का महत्व
गायत्री मंत्र वेदों का सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इस सार्वभौमिक मंत्र-प्रार्थना का उल्लेख सभी चार वेदों के साथ-साथ तंत्रों में भी किया गया है (तंत्र हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। तंत्र को वेदों का गूढ़ हिस्सा माना जाता है - कलियुग के वेद। तंत्रों में) मंत्रों का विज्ञान सबसे अधिक गहराई से विकसित है - मंत्र-शास्त्र। "शास्त्र" शब्द का अर्थ है "ग्रंथ"। महान ऋषि-मुनि उसकी अत्यंत प्रशंसा करते हैं। जैसा कि श्री सत्य साईं बाबा कहते हैं, यह बिना किसी अपवाद के सभी लोगों के लिए है, चाहे उनकी जाति, धर्म, निवास स्थान और विकास का स्तर कुछ भी हो। उनमें सभी वेदों का सार समाहित है, और इसलिए उन्हें वास्तव में वेदों की माता कहा जाता है। जिस प्रकार वेदों की शिक्षाओं का सार उपनिषदों (वेदों के दार्शनिक भाग) में निहित है, उसी प्रकार उपनिषदों का सार गायत्री मंत्र में निहित है। चारों वेदों में से प्रत्येक एक मूल सत्य की पुष्टि करता है: प्रज्ञानं ब्रह्म (चेतना ही ब्रह्म है) - ऋग्वेद; अहं ब्रह्मा अस्मि (मैं ब्रह्म हूं) - यजुर्वेद; तत् त्वम् असि (आप वही हैं) - स्वयं वेद; अयं आत्मा ब्रह्म (यह आत्मा ही ब्रह्म है) - अथर्ववेद। जब ये चारों सत्य मिल जाते हैं तो गायत्री प्रकट होती है। दावा किया जाता है कि अगर इसका नियमित पाठ किया जाए तो इसका प्रभाव वेदों के पाठ के समान ही लाभकारी होगा।
गायत्री मंत्र का अत्यधिक महत्व हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक - "उपनयन" में परिलक्षित होता है। उपनयन लड़कों के लिए "दीक्षा" का एक संस्कार है, जब उन्हें प्रशिक्षुता की अवधि के लिए एक शिक्षक (गुरु) के घर लाया जाता था। इस अनुष्ठान का एक तत्व गायत्री मंत्र की दीक्षा है। इसके बाद, दीक्षार्थी "दो बार जन्मा" बन जाता है। गुरु से गायत्री मंत्र प्राप्त करना, इस संस्कार के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक के रूप में, एक व्यक्ति के सचेत आध्यात्मिक विकास के पथ पर प्रवेश का प्रतीक है, अर्थात उसका "दूसरा" आध्यात्मिक जन्म।
जिस प्रकार पदार्थ में अवतरण की प्रक्रिया ईश्वर के शब्दों "एको "हं बहु स्याम" - "मैं एक हूं" के साथ एकता को अनेक में विभाजित करने से शुरू होती है। क्या मैं अनेक हो सकता हूँ!", ईश्वर के साथ मिलन की प्रक्रिया "भर्गो देवस्य धीमहि" शब्दों से शुरू होती है - "हम दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं!"
ऋषियों और मन्त्र का आकार
आमतौर पर, महत्वपूर्ण वैदिक मंत्रों का पाठ सहायक - विनियोग मंत्रों के पाठ से पहले किया जाता है, जो ऋषि, आकार, देवता और उद्देश्य को इंगित करता है जिसके लिए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है।
गायत्री से संबंधित विनियोग मंत्र में बताया गया है कि गायत्री मंत्र के मुख्य भाग के ऋषि विश्वामित्र हैं। कुछ लोग उनकी पहचान पुराणों (हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों) में वर्णित प्रसिद्ध ऋषि से करते हैं। हालाँकि, प्रोफेसर तैमनी के अनुसार, यह गायत्री मंत्र के उच्च उद्देश्य के अनुरूप नहीं है, जिसे वेदों की माता माना जाता है। "विश्वामित्र" ब्रह्माण्ड के रचयिता ब्रह्मा का एक नाम है और वही इस मन्त्र के ऋषि हैं।
गायत्री मन्त्र का मुख्य भाग एक छंद में लिखा हुआ है जिसका नाम भी यही है-गायत्री। इसमें चौबीस अक्षर हैं, जो आठ-आठ अक्षरों की तीन पंक्तियों में व्यवस्थित हैं। यह आकार प्राचीन और पवित्र माना जाता है।
मंत्र के उद्देश्य या प्रयोजन की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। जहां तक देवता गायत्री मंत्र का सवाल है, विनियोग मंत्र कहता है कि यह सविता है।
हमारे ब्रह्मांड का सवितार या ईश्वर
इस मंत्र का दूसरा नाम "सविता गायत्री" या "सावित्री" (अंतिम अक्षर पर जोर देने के साथ) है। यहां फिर कुछ भ्रम है. संयोजन "सविता गायत्री" का शाब्दिक अर्थ है "गायत्री सवितार", जहां "सविता" (मर्दाना) शब्द की व्याख्या "सविता का देवता" के रूप में की जा सकती है। इस शब्द का एक पर्यायवाची शब्द इसका दूसरा रूप है - शब्द "सावित्री" (सावित्र-आर-आर की तरह लगता है; यह अंत में तथाकथित शब्दांश "आर" के साथ पुल्लिंग भी है, जिसमें लघु "आई" के समान एक स्वर है ”), जो कि 'सावित्री' शब्द के साथ भ्रमित है, जिसका अर्थ मंत्र है। इस शब्द (स्त्रीलिंग) के अंत में एक लंबा और तनावग्रस्त "मैं" है और, फिर से, यह देवी गायत्री का दूसरा नाम है।
मंत्र कहता है, "हम सविता के दिव्य प्रकाश पर ध्यान करते हैं।" सवितार अपने उच्चतम पहलू में सूर्य देवता है। सूर्य का प्रकाश या सवितार (और स्वयं सवितार नहीं) उनकी शक्ति है, यानी देवी सवित्री या गायत्री। इसलिए, मंत्र को एक साथ सावित्री (देवी गायत्री) और सवितार - देवता या मंत्र के अध्यक्ष देवता दोनों को संबोधित किया जाता है।
भोर से सूर्यास्त तक सूर्य को सूर्य कहा जाता है। भोर से पहले का सूर्य, जो सजीव या जीवनदायी शक्ति का प्रतीक है, सविता कहलाता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकट प्रकाश का आधार भोर से पहले के सूर्य की "जीवित करने वाली शक्ति" है, जो इसकी अभिव्यक्ति को संभव बनाती है, उसी प्रकार सूर्य के अस्तित्व का आधार सविता है। उत्तरार्द्ध हमारे ब्रह्मांड का सर्वोच्च आध्यात्मिक सार है - भगवान या (हिंदू शब्दावली में) ईश्वर।
मंत्र में वह स्वयं ब्रह्म को व्यक्त करता है। जैसा कि श्री सत्य साईं बाबा कहते हैं: "अंतर्निहित और पारलौकिक देवता, जिसे सवितार कहा जाता है, जिसका अर्थ है "जिससे सब कुछ पैदा होता है" ... अर्थात, जिस सत्ता को गायत्री को संबोधित किया जाता है वह वास्तव में स्वयं ब्रह्म है" (धर्म वाहिनी देखें) ).
भारतीय दर्शन के अनुसार, केवल एक ही सर्वोच्च वास्तविकता है - ब्राह्मण (यूरोपीय दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं में इसे क्रमशः पूर्ण या ईश्वर कहा जाता है)। अव्यक्त स्तर पर, यह सर्वोच्च वास्तविकता (निर्गुण ब्रह्म) चेतना और शक्ति की एक अविभाज्य एकता है। जब यह वास्तविकता बाहर की ओर (सगुण ब्रह्म के रूप में) प्रकट होने लगती है, तो चेतना और शक्ति में एक प्राथमिक भेदभाव होता है, जिसे तांत्रिक शब्दावली में शिव और शक्ति कहा जाता है। शक्ति को प्रकट ब्रह्मांड में किए जाने वाले कार्यों की बहुलता के अनुरूप असंख्य शक्तियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक बल चेतना के एक विशेष कार्य से मेल खाता है, जो ब्रह्मांड में होने वाली बुनियादी प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। ये कार्य और शक्तियां, एक सर्वोच्च ईश्वर - ब्राह्मण के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, हिंदू धर्म के देवता या देवता हैं।
विशाल ब्रह्मांड में कई छोटे ब्रह्मांड या सौर मंडल हैं। सर्वोच्च देवता, या यूं कहें कि किसी भी ब्रह्मांड का भगवान, ईश्वर है। प्रत्येक सौर मंडल या ब्रह्माण्ड ब्रह्मांड की एक अलग आत्मनिर्भर इकाई है और ईश्वर द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामक अपने तीन पहलुओं पर शासन किया जाता है, जिनका मुख्य कार्य सृजन, रखरखाव और विघटन है। अपने उच्चतम पहलू में, रुद्र को महेश या महेश्वर कहा जाता है। रुद्र और महेस दोनों की पहचान शिव से की जाती है, या यूं कहें कि वे प्रकट स्तर पर उनके कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि प्रकट स्तर पर रुद्र रूपों को नष्ट करने का कार्य करता है, तो महेश किसी भी रूप की अभिव्यक्ति के अंतर्निहित चेतना के शुद्ध कार्य से मेल खाता है। इस पहलू में, वह व्यावहारिक रूप से ईश्वर से अलग नहीं है, जिसका मुख्य कार्य "नियंत्रण" के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
"भौतिक सूर्य के अंदर," जैसा कि प्रोफेसर अपनी पुस्तक "गायत्री" में लिखते हैं। आई. के. तैमनी (पृ. 88), - पूरे सौर मंडल में व्याप्त, असाधारण वैभव और शक्ति के कई अदृश्य संसार हैं, और वे सभी शक्तिशाली सत्ता की अभिव्यक्ति या शरीर हैं जिन्हें सौर लोगो या सूर्य नारायण कहा जाता है। यह प्राणी हमारे ब्रह्मांड का ईश्वर या ईश्वर है। हमारे सौर मंडल में चेतना के सभी रूप उनकी चेतना की सीमित अभिव्यक्तियाँ हैं। सभी शक्तियाँ उसकी शक्ति की व्युत्पन्न हैं।
ईश्वर की शक्ति के रूप में गायत्री देवी
वैदिक काल से ही गायत्री मंत्र को देवी गायत्री या गायत्री देवी का स्वरूप माना गया है। प्रोफ़ेसर के अनुसार इसका प्रतीकवाद। तैमनी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के समान है, एकमात्र अंतर यह है कि यह एक भगवान की महिला हाइपोस्टेसिस की त्रिमूर्ति है। "इसमें कोई संदेह नहीं है," वे लिखते हैं (उक्त, पृ. 23-24) "कि ये तीन महिला रूप उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो साधक को इन तीन देवताओं की चेतना के साथ एकता प्राप्त करने की अनुमति देती है। गायत्री के तीन रूपों का प्रकट ब्रह्मांड में उनके सामान्य कार्यों के रूप में प्रकट तीन देवताओं की शक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। ये तीन शक्तियाँ या शक्तियाँ, जिन्हें आमतौर पर सृजन, संरक्षण और विनाश की शक्तियाँ कहा जाता है, देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली द्वारा व्यक्त की जाती हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र (शिव) की पत्नी या शक्ति कहा जाता है। इस प्रकार, यदि कोई साधक ज्ञान या विद्या प्राप्त करना चाहता है, तो वह सरस्वती की पूजा करता है; यदि वह सांसारिक मामलों में धन और सौभाग्य चाहता है, तो वह लक्ष्मी की पूजा करता है; यदि वह दुर्भाग्य में मदद मांगता है, तो वह काली को बुलाता है।
हालाँकि, अगर वह कुछ भी नहीं चाहता है जो ये तीन देवता अपनी-अपनी शक्तियों के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन स्वयं ईश्वर को (एहसास) करने की इच्छा रखता है, तो उसे गायत्री की ओर मुड़ना चाहिए, क्योंकि वह उसकी चेतना के साथ मिलन प्राप्त करने की शक्ति है और इस तरह - उसे जानो।" इस प्रकार, गायत्री देवी स्वयं ईश्वर की शक्ति हैं। इसलिए उनमें ऐसी शक्ति है!
मंत्र का अर्थ और प्रतीकवाद
कई अन्य पवित्र चीज़ों की तरह, गायत्री मंत्र में भी समृद्ध प्रतीकवाद और व्याख्या के कई स्तर हैं। गायत्री मंत्र के कई अनुवाद हैं। व्याख्या के भौतिक स्तर पर, सवितार को भौतिक सूर्य के रूप में समझा जाता है, जिसे देवता के रूप में दर्शाया जाता है, और इसकी रोशनी और ऊर्जा को भी विशुद्ध भौतिक अर्थ में समझा जाता है। तब मंत्र के शब्दों का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है "हम सूर्य की उज्ज्वल चमक का चिंतन करते हैं!" यह हमें सच्ची समझ प्रदान करे!” या "यह हमें सत्य के मार्ग पर मार्गदर्शन करे!" व्याख्या के उच्च स्तर पर, जब सवितार शब्द का अर्थ सर्वोच्च चेतना या स्वयं ईश्वर (ईश्वर) है, और उसके प्रकाश का अर्थ उसकी शक्ति, महानता और महिमा है, उदाहरण के लिए, मंत्र का अर्थ यह हो सकता है: "परमात्मा पर" ईश्वर की महिमा, सर्वोच्च श्रद्धा के योग्य, आइए हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें! क्या वह हमारे मन को प्रकाशित कर सकता है!” या "वह हमें आत्मज्ञान प्रदान करें!" आप इन दोनों अर्थों को एक साथ जोड़कर अधिक विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं: "हम सूर्य की उज्ज्वल रोशनी पर ध्यान करते हैं (सवितार की दिव्य शक्ति और महिमा का प्रतीक, जो सभी पूजा का सर्वोच्च लक्ष्य है और ईश्वर स्वयं) ! वह हमें आत्मज्ञान प्रदान करें!” शब्द "भूर् - भुवः - स्वः" का अनुवाद या तो किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, "ओम!" धरती! हवाई क्षेत्र और आकाश! या: "सांसारिक, सूक्ष्म और दिव्य दुनिया के लिए अच्छा है!", या अनुवाद के बिना रहें। ये पवित्र शब्द हैं, जिनके बारे में हम नीचे बात करेंगे।
इस मंत्र के मुफ़्त अनुवाद भी हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, जॉन वुड्रोफ ने अपनी पुस्तक "तंत्र शास्त्र का परिचय" में "गायत्री मंत्र" अध्याय में निम्नलिखित अनुवाद दिया है: "ओम! आइए हम सांसारिक, वायु और स्वर्गीय क्षेत्रों के दिव्य निर्माता की अद्भुत आध्यात्मिक प्रकृति पर चिंतन (ध्यान) करें! क्या वह हमारे विचारों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उपलब्धि की ओर निर्देशित कर सकते हैं! ”, जहां अंतिम शब्द (मानव सांसारिक अस्तित्व के चार लक्ष्य) बस जोड़े गए हैं, हालांकि, सामान्य तौर पर, यह अर्थ का खंडन नहीं करता है। वहाँ केवल काव्यात्मक अनुवाद भी होते हैं, जिनमें मुख्य बात शब्दों के अर्थ को बिल्कुल सटीक रूप से व्यक्त करना नहीं है, बल्कि भाषा की सुंदरता का उपयोग करके मंत्र की भावना को व्यक्त करना है। यहाँ उनमें से एक है: “हे पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के दिव्य स्रोत! अपनी अनगिनत किरणों में से, मुझे एक प्रदान करें, ताकि मेरे जीवन में, कम से कम एक पल के लिए, मैं आपकी तरह चमक सकूं!” सिद्धांत रूप में, अधिकांश अनुवाद सही हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर वे मंत्र के मुख्य विचार को समझने के एक या दूसरे पहलू को सही ढंग से दर्शाते हैं। मंत्र के सार में प्रवेश की डिग्री, निश्चित रूप से, उस व्यक्ति के आध्यात्मिक अनुभव, ज्ञान और विकास के स्तर पर निर्भर करती है जो इसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहा है। गायत्री मंत्र के अर्थ और महत्व की गहराई उतनी ही असीम और अक्षय है जितनी कि वह दिव्य स्रोत जिसकी यह अभिव्यक्ति है।
यह मंत्र अपनी संरचना में भी गहरा प्रतीकात्मक है। इसे तीन, पाँच और नौ भागों में बाँटा जा सकता है। जैसा कि श्री सत्य साईं बाबा बताते हैं, इस मंत्र के पहले 9 शब्द सर्वोच्च वास्तविकता का नौ गुना वर्णन हैं।
1. ॐ- मौलिक ध्वनि कंपन जो सृष्टि का आधार है; ब्रह्म का प्रतीक, साथ ही ईश्वर का भी;
2. भूर- भूर-लोक; अस्तित्व का सांसारिक स्तर; सांसारिक संसार, सघन भौतिक पदार्थ और ब्रह्मा से संबंध रखता है;
3. भुवः- भुवर-लोक; अस्तित्व का ईथर तल; सूक्ष्म (सूक्ष्म) जगत से भी संबंध रखता है; ईथर और सूक्ष्म पदार्थ, साथ ही विष्णु के साथ;
4. दियासलाई बनानेवाला-स्वर (गा)-लोक; अस्तित्व का स्वर्गीय स्तर; दिव्य (आकस्मिक) दुनिया, मानसिक और कारण स्तरों के पदार्थ, महेश्वर के साथ भी संबंध रखता है;
5. गूंथना- वह (नाम पर); सर्वोच्च वास्तविकता, शब्दों में अवर्णनीय, और इसलिए केवल एक संकेतवाचक सर्वनाम द्वारा निर्दिष्ट; ब्रह्म, पूर्ण; भी<здесь>- टोगो पर (वि. पैड.); ब्रह्म और ईश्वर दोनों से संबंधित हो सकता है;
6. सवितुर- सवितार (सवितार से जन्मा); सूर्य के भौतिक आवरण के पीछे छिपी जीवनदायिनी शक्ति, ईश्वर का प्रतीक है, जो बदले में स्वयं ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है;
7. जाम- इच्छित; सभी आकांक्षाओं और श्रद्धा के योग्य (मोडल विशेषण या कर्तव्य विशेषण);
8. भरगो- चमक; प्रकाश (दिव्य चेतना); वैभव; इसे शिव की शक्ति के साथ-साथ ईश्वर की शक्ति के साथ भी जोड़ा जा सकता है; वह है, गायत्री देवी;
9. कुँवारी- दिव्य, दीप्तिमान, अनुग्रह प्रदान करने वाला (जीनस पतन। या देव से विशेषण)।
शेष शब्द, तीन समूहों में विभाजित, पहले नौ शब्दों के साथ, मंत्र की 12 सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं:
10. धिमाही- ध्यान करें; चिंतन (क्रिया 3 शाब्दिक बहुवचन में);
11. धियो- कारण, बुद्धि, मन; यो- वह कौन;
12. नः- हमारा; प्रचोदयात्- क्या वह (सच्चाई के मार्ग पर) मार्गदर्शन कर सकता है; क्या यह रोशन हो सकता है! क्या वह आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है! (उपवाचक).
प्रतीकात्मक रूप से, देवी गायत्री को पांच सिरों, यानी पांच मुखी (पंच मुखी) के साथ दर्शाया गया है। साईं बाबा के अनुसार, इसके पांच चेहरे या पहलू, मंत्र के पांच भागों के साथ-साथ पांच विराम (प्राणायाम) के अनुरूप हैं।
नीचे हम मूल शब्दों के क्रम को ध्यान में रखते हुए, शाब्दिक (शब्द-दर-शब्द) अनुवाद के साथ मंत्र के पांच गुना विभाजन के साथ आते हैं:
1. ओम!
2. भूर् भुवः स्वाहा- भूर, भुवर, स्वर-लोकी!
3. तत् सवितुर जाम- उस सवितार की इच्छा के लिए
4. भर्गो देवस्य धीमहि- आइये दिव्य प्रकाश का ध्यान करें!
5. धियो यो नः प्रचोदयात्- क्या वह हमारे मन को प्रकाशित कर सकता है!
गायत्री देवी के पांच चेहरे स्वयं ईश्वर को प्रकट और प्रतिबिंबित करते हैं। वे 5 प्रकार की ऊर्जा (प्राण) उत्सर्जित करते हैं और 5 स्थूल (भूत) और 5 सूक्ष्म (तन्मात्रा) तत्वों, मानव शरीर के 5 कोषों (कोशों), 5 अनुभूति अंगों (ज्ञान-इंद्रिय) और 5 कर्म अंगों ( कर्म-इंद्रिय). इन सभी घटकों को नियंत्रित करके, गायत्री देवी पूरी तरह से संपूर्ण मानव जाति में व्याप्त हो जाती है और मंत्र का उच्चारण करते समय, उपरोक्त सभी तत्वों को शुद्ध और परिवर्तित करने में सक्षम होती है। इसलिए इस मंत्र का महत्व और शक्ति!
जैसा कि श्री सत्य साईं बाबा बताते हैं, गायत्री मंत्र को भी तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। उनमें से प्रत्येक का अपना नाम है, अर्थात्:
1. वर्ण - मंत्र के वर्ग को परिभाषित करना और मंत्र को नियंत्रित करने वाली उच्च शक्तियों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति को दर्शाता है;
2. ध्यान - एकाग्रता की वस्तु का संकेत - ध्यान;
3. प्रार्थना - यह दर्शाता है कि मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति क्या मांगता है - प्रार्थना।
मंत्र के प्रत्येक भाग का अपना लक्ष्य होता है, जो मंत्र के अन्य भागों के लक्ष्य से जुड़ा होता है। ये लक्ष्य प्रोफेसर आई.के. तैम्नी द्वारा स्पष्ट रूप से तैयार किए गए हैं (उक्त - पृ. 70−71):
गायत्री मंत्र के पहले भाग का उद्देश्य साधक के वाहनों में कुछ कंपन पैदा करना और उन शक्तियों को सक्रिय करना है जो मंत्र के दूसरे और तीसरे भाग की प्रभावी कार्रवाई के लिए जमीन तैयार करेंगे।
मंत्र के दूसरे भाग का उद्देश्य साधक के मन में सविता-ईश्वर की चेतना के संपर्क में आने के लिए एक मजबूत आकांक्षा और दृढ़ संकल्प पैदा करना है और इस तरह उसके आध्यात्मिक दिमाग के खुलने की प्रक्रियाओं को उत्तेजित करना है। इस तथ्य के बावजूद कि साधक की चेतना पहले से ही सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा है, निचले स्तर की सीमाओं के कारण, इस एकता की जागरूकता खो जाती है। साधक अपने संकल्प द्वारा उसे पुनः खोजने का प्रयास करता है।
मंत्र के तीसरे भाग का उद्देश्य मंत्र के अभ्यासी में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना पैदा करना है, जो दैवीय कृपा के अवतरण के लिए नितांत आवश्यक है। गहन अभीप्सा के बाद, जिसमें साधक की चेतना सक्रिय भूमिका निभाती है, वह खुद को पूरी तरह से भगवान की दया के सामने समर्पित कर देता है और निष्क्रिय हो जाता है और उसमें शामिल उच्च शक्तियों के प्रति खुला हो जाता है।
आई. ॐ भूर् भुवः स्वः!
मंत्र के पहले भाग में पवित्र शब्दांश ओम या प्रणव ("प्र" + "नु" से - "कंपन करना, ध्वनि बनाना") और तीन रहस्यमय शब्द-मंत्र शामिल हैं जिन्हें महाव्याहृति कहा जाता है: भूर - भुवः - स्वाह। उत्तरार्द्ध प्रणव से उत्पन्न हुए हैं और इसके विभेदित रूप हैं। ओम व्यक्तिगत जीवात्मा (मनुष्य में दिव्य आत्मा) और परमात्मा (ब्रह्मांड में दिव्य आत्मा) के बीच संबंध को व्यक्त करता है और ईश्वर का मंत्र है। जिस तरह हमारे ब्रह्मांड का निर्माण पवित्र ध्वनि "ओम" के उच्चारण से हुआ था, उसी तरह तीन महाव्याहृतियों के उच्चारण से, तीन निचले लोक या अस्तित्व के स्तर (भौतिक, सूक्ष्म और मानसिक) का निर्माण हुआ। इस संपूर्ण संयोजन का समग्र रूप से एक पवित्र चरित्र है, क्योंकि ये शब्द क्रमशः बीज मंत्रों और उन्हें नियंत्रित करने वाले देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: ईश्वर, अग्नि, वायु और आदित्य, जो कि विनियोग मंत्र में कहा गया है। यह चार शब्द की अभिव्यक्ति प्रत्येक ब्राह्मण द्वारा प्रार्थना की शुरुआत में बोली जाती है और सर्वोच्च वास्तविकता के समक्ष अभिवादन और आराधना की अभिव्यक्ति के बराबर है। इन पवित्र शब्दों का उच्चारण करके, मंत्र का पाठक, मानो, मानसिक रूप से निर्माता (ओम) और संपूर्ण सृष्टि (तीन लोक जिनमें आत्मा अवतारों के चक्र से गुजरती है) से जुड़ जाता है और उनके सामने झुक जाता है।
द्वितीय. तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि!
दूसरे भाग में, मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति यह याद करते हुए कि किसी भी मानवीय आकांक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर (ईश्वर) है, उसकी असीम महानता, महिमा और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है और मानसिक रूप से उसके साथ जुड़ता है। साथ ही, वह कल्पना करता है कि कैसे सूर्य की दीप्तिमान रोशनी (अपनी शक्ति के माध्यम से) के माध्यम से इस सर्वोच्च सत्ता की कृपा उस पर प्रवाहित होती है।
यहां "धीमहि" शब्द पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिसका बहुवचन है - "ध्यान"। यह इंगित करता है कि साधक न केवल अपने कल्याण की परवाह करता है और पूरी तरह से स्वार्थी लक्ष्यों का पीछा नहीं करता है, बल्कि सभी जीवित प्राणियों की ओर से अभ्यास करता है। इस शब्द का अनुवाद दो तरह से किया जा सकता है: "आओ ध्यान करें" और "हम ध्यान करें" के रूप में। पहले मामले में, वाक्य में इच्छा का अर्थ होता है और प्रार्थना बन जाता है। दूसरे मामले में यह एक प्रतिज्ञान है और साधक के सर्वोच्च सत्ता के संपर्क में आने के दृढ़ संकल्प को व्यक्त करता है, जो ध्यान के अर्थ में समझे जाने वाले इस भाग के अर्थ के अनुरूप है।
तृतीय. धियो यो नः प्रचोदयात्!
मंत्र का तीसरा भाग वास्तविक प्रार्थना या अनुरोध-इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उच्चारणकर्ता ईश्वर से अपने मन (बुद्धि) की रोशनी के माध्यम से अपने दिव्य स्वभाव को जागृत करते हुए, उसे आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए कहता है। दूसरे भाग की तरह, इस वाक्य में "प्रचोदयात्" शब्द की दोहरी व्याख्या है: "वह (जो) हमारे मन को प्रकाशित करता है!" और कैसे "वह हमारे मनों को प्रकाशित करे!" ऊपर जो कहा गया है उसके आधार पर (चूँकि यह प्रार्थना की भावना से अधिक सुसंगत है), दूसरा विकल्प अधिक स्वीकार्य है। शब्द "धियास" (ध्वनियों के विलय के नियमों के अनुसार, "धियो" में बदल गया) बहुवचन में भी है और इसका शाब्दिक अर्थ है "हमारा मन", यह दर्शाता है कि साधक भगवान से न केवल अपने लिए, बल्कि अपने लिए भी दया की प्रार्थना करता है। सभी लोग।
वैसे, हिंदू धर्म का यह मुख्य मंत्र-प्रार्थना और सार्वभौमिक खुशी के लिए एक और दैनिक दोहराया प्रार्थना; “सर्वे जन सुखिनो भवन्तु! लोक समस्ता सुखिनो भवन्तु!", जिसका अर्थ है "सभी संसार के सभी प्राणी खुश रहें!" (शाकाहार और सच्ची धार्मिक सहिष्णुता के साथ) हिंदू धर्म को एक अत्यधिक परोपकारी विश्व धर्म के रूप में चित्रित किया गया है। श्री सत्य साईं बाबा कहते हैं कि यह सर्वोच्च धर्म है, जिसमें अन्य सभी शामिल हैं (सत्य साईं वाहिनी देखें)।
मंत्र की त्रिमूर्ति और त्रिमूर्ति के प्रतीकवाद को कई स्तरों पर खोजा जा सकता है। तीन ध्वनियों (ए-यू-एम), पवित्र शब्दांश ओम, तीन महाव्याहृति और मंत्र के तीन भागों से मिलकर एक दूसरे के साथ और अन्य पवित्र त्रय के साथ सहसंबद्ध हैं: हिंदू त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, शिव-महेश्वर), तीन गुण (सत्त्व, रजस, तमस), समय की तीन अवधि (अतीत, वर्तमान, भविष्य), प्राणायाम के तीन चरण (साँस लेना, रोकना, छोड़ना), चेतना की तीन अवस्थाएँ (जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति), तीन शरीर (स्थूल-, सूक्ष्म- और) करण-शरीरा), शास्त्रों के तीन पहलू (तंत्र, मंत्र और यंत्र), तीन पवित्र अग्नि (गार्हपत्य, दक्षिणा, आहवनिया), आदि।
कई मामलों में, त्रिमूर्ति जो सृष्टि के प्रकट स्तर पर हावी है, एक चौथे, अधिक आवश्यक, अव्यक्त पहलू (पीड़ा - ओम की ध्वनि की निरंतरता के रूप में मौन की अश्रव्य ध्वनि; ईश्वर, हिंदू त्रिमूर्ति को एकजुट करती है; तुरिया) की ओर इशारा करती है और इंगित करती है। - चेतना की चौथी अवस्था, अन्य सभी से श्रेष्ठ, आदि ...; यहां चौथी के रूप में स्वयं गायत्री हैं - तीन शक्तियों की संश्लेषण शक्ति)।
त्रिमूर्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिसके साथ गायत्री जुड़ी हुई है, तीन संध्याएं हैं, यानी दिन के तीन संक्रमणकालीन समय (भोर, दोपहर, सूर्यास्त), जो संक्रमणकालीन अवस्थाओं का प्रतीक हैं।
सुबह की संध्या एक ओर देवी के मुख्य नाम - गायत्री, और दूसरी ओर - शक्ति ब्रह्मा (ब्राह्मणी) के साथ-साथ ऋग्वेद से संबंधित है। मध्याह्न संध्या का संबंध सावित्री नाम और शक्ति विष्णु (वैष्णवी) के साथ-साथ यजुर्वेद से भी है। शाम की संध्या का संबंध सरस्वती नाम और रुद्र की शक्ति (रुद्राणी) के साथ-साथ सामवेद से भी है। इसके अलावा, ये तीन संध्याएँ, गायत्री की आवश्यक प्रकृति के कारण, स्वयं चौथी - संक्रमणकालीन अवस्था का प्रतीक हैं। संक्रमणकालीन अवस्थाएँ (नींद और जागरुकता के बीच, जीवन और मृत्यु, दो विचारों के बीच का अंतर, ऊर्जाओं की क्रिया में परिवर्तन का क्षण - तत्व, आदि) आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह वह दृश्य शून्य है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। यह कोई संयोग नहीं है कि साईं बाबा नींद और जागने के बीच की स्थिति पर ध्यान करने की सलाह देते हैं। इन अवस्थाओं की प्रकृति को जानना ब्रह्म की प्रकृति को जानने के समान है। गायत्री मंत्र इन संक्रमणकालीन अवस्थाओं को नियंत्रित करता है और इसीलिए यह आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है, अर्थात अज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर संक्रमण।
मंत्र साधना और उसका प्रभाव
“गायत्री मंत्र का जाप सुबह, दोपहर और शाम के समय करना चाहिए... सुबह या शाम के समय इसका जाप करना नितांत आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो कुछ उद्देश्यों के लिए इसे दोपहर के समय भी पढ़ा जा सकता है। यदि आप मंत्र जप को साधना मानते हैं, तो सुबह और शाम का समय सबसे पवित्र है, ”साईं बाबा कहते हैं, यह बताते हुए कि सुबह 4 से 8 बजे और सुबह 4 से रात 8 बजे तक का समय सात्विक है। हालाँकि, इस मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है: स्नान के दौरान, खाने से पहले, रात में।
इसे कम से कम 3 बार दोहराया जाना चाहिए। साईं बाबा खाना खाने से पहले उसे 3, 9 या 11 बार पढ़ने की सलाह देते हैं। जप करने वालों के लिए, दोहराव की पारंपरिक संख्या (जप का एक "चक्र") 108 बार है, हालाँकि यहाँ कोई सीमा नहीं हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि मंत्र की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए यह संख्या न्यूनतम है।
जप का अभ्यास करने के लिए, आपको एक शांत जगह का चयन करना चाहिए, आरामदायक स्थिति में बैठना चाहिए, अपनी रीढ़ को सीधा रखना चाहिए, और मानसिक रूप से "बुद्ध क्रॉस" बनाना चाहिए, अर्थात, "सभी प्राणियों को शांति" के विचार को सभी दिशाओं में तीन बार (आगे) भेजना चाहिए , पीछे, बाएँ, दाएँ, ऊपर और नीचे)। सभी प्राणियों को खुशी! सभी प्राणियों को ख़ुशी!” इसके बाद, आप गणेश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मंत्रों का पाठ कर सकते हैं (क्योंकि कोई भी कार्य केवल उनकी अनुमति से ही सकारात्मक परिणाम ला सकता है): ओम श्री गणेशाय नमः!, सभी गुरुओं को (ओम श्री गुरुभ्यो नमः), साथ ही सभी देवताओं को (ओम श्री देवेभ्यो नमः), जिसका अर्थ है "मैं गणेश, सभी गुरुओं और देवताओं के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता हूं!" फिर आपको अपने पैर की उंगलियों से लेकर सिर के शीर्ष तक और इसी तरह ऊपर से नीचे तक सभी मांसपेशियों को आराम देना चाहिए। इसके बाद आप कल्पना करें कि आपके गुरु आपके सिर के ऊपर बैठे हैं। उन्हें संबोधित करते हुए, गुरु मंत्र बोलें: गुरुर ब्रम्हा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराह गुरु साक्षात परम ब्रम्हा तस्मै श्री गुरवे नमः, जिसका अर्थ है "गुरु ब्रह्मा हैं; गुरु विष्णु हैं; गुरु भगवान महेश्वर हैं! गुरु स्वयं परब्रह्म हैं! ऐसे गुरु की मैं पूजा करता हूं" . फिर आपको अपनी छाती के मध्य में या अपने सामने एक प्रकाश स्रोत (सौर डिस्क) की कल्पना करनी चाहिए, जो अपनी चमक फैला रहा है, और इस स्रोत के केंद्र में देवी गायत्री की छवि है (कवर पर देखें)। इसके बाद आप जप शुरू कर सकते हैं।
जप माला पर भी किया जा सकता है, विशेषकर 108 मनकों वाली माला पर। मोतियों को अंगूठे और मध्यमा उंगली का उपयोग करके घुमाना चाहिए। अंगूठा ब्राह्मण के लिए, तर्जनी जीव के लिए, और अन्य तीन गुण के लिए: मध्यमा उंगली सत्व के लिए, अनामिका रजस के लिए और छोटी उंगली तमस के लिए है। माला को मध्यमा उंगली पर लटकाकर जीव को गुणों से अलग करना चाहिए। आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और मध्यमा उंगलियों से मोतियों पर अंगुली रखनी चाहिए। तर्जनी का सिरा अंगूठे को छूता है। यह जीव की देव में विलय की इच्छा का प्रतीक है। माला पर एक और 109वां मनका होता है, जो आमतौर पर आकार में बड़ा होता है। वह शेष 108 मनकों को साझा करती है और गुरु कहलाती है। जप का अभ्यास करते समय, आप इस पर छलांग नहीं लगा सकते। वहां पहुंचकर आपको माला को पलट देना चाहिए और विपरीत दिशा में गिनना शुरू कर देना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति जो मंत्र का अभ्यास करना चाहता है उसका मन बहुत बेचैन है, तो सबसे अच्छा है कि वह मंत्र को जोर से दोहराना शुरू कर दे। फिर थोड़ी देर के बाद आप चुपचाप और चुपचाप मंत्र दोहराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मंत्र को धीरे-धीरे और मानसिक रूप से दोहराते समय, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मन विचलित न हो और पुनरावृत्ति यांत्रिक न हो। हालाँकि, किसी मंत्र को दोहराते समय सबसे महत्वपूर्ण बात मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता है।
मंत्र की शक्ति पर विश्वास भी बहुत जरूरी है। साईं बाबा कहते हैं, "चूँकि गायत्री ईश्वरीयता का पर्याय है," साईं बाबा कहते हैं, "इसके साथ विनम्रता और श्रद्धा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए: मंत्र के प्रति प्रेम और श्रद्धा और वादा किए गए परिणाम में विश्वास, मन भटकते समय यांत्रिक दोहराव से अधिक महत्वपूर्ण है... प्रदर्शन करें यह ईश्वर की पूजा है"
मंत्र के सही उच्चारण को महत्व दिया जाता है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण स्पष्ट और स्पष्ट रूप से, रुक-रुक कर, उचित लय और सही स्वर-शैली का ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए। किसी मंत्र का सही उच्चारण करने के लिए, आपको उसकी टेप रिकॉर्डिंग का उपयोग करना चाहिए, बस उसकी ध्वनि को कान से पुन: उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इसका ध्वन्यात्मक अंकन इसमें सहायता कर सकता है।
नीचे हम गायत्री मंत्र को स्वर और उच्चारण के पदनाम के साथ प्रस्तुत करते हैं जैसा कि श्री सत्य साईं बाबा ने उच्चारण किया था। स्पष्टीकरण बताता है कि कुछ संकेतों का क्या मतलब है, साथ ही कुछ ध्वनियों का उच्चारण कैसे किया जाए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिए गए नोटेशन पूरी तरह से संस्कृत शब्दों के प्रसारण के सटीक नियमों के अनुरूप नहीं हैं, लेकिन रूसी बोलने वालों की समझ की सुविधा के लिए यहां दिए गए हैं:

स्पष्टीकरण:
1. किसी पंक्ति की शुरुआत से पहले एक क्षैतिज रेखा मौलिक स्वर को इंगित करती है।
2. एक घुंघराले ब्रैकेट, जिसकी नोक मौलिक स्वर के स्तर को भी इंगित करती है, एक विराम को चिह्नित करती है।
3. एक रेखा का ऊर्ध्वाधर बदलाव दो अर्धस्वर (या एक स्वर) के बराबर होता है, जैसा कि कुंजी में दिखाया गया है: जहां "0" मूल स्वर है, ऊपर और नीचे "2" संबंधित रेखा के स्वर में बदलाव को दर्शाता है 2 सेमीटोन ऊपर या नीचे से।
4. अक्षर (U, I) के ऊपर की पट्टी स्वर की लंबाई को इंगित करती है; "ई/ई" और "ओ" ध्वनियाँ हमेशा लंबी होती हैं, हालाँकि उनका देशांतर आमतौर पर इंगित नहीं किया जाता है। ध्वनि "ई/ई" अंग्रेजी "ई" के समान है और इसे रूसी "ई" और "ई" के बीच एक क्रॉस की तरह उच्चारित किया जाता है, जो बाद वाले के करीब है।
5. बीएक्स, डीएक्स के संयोजन में छोटा "एक्स", एक महाप्राण "एक्स" को दर्शाता है, जो बहुत कमजोर लगता है।
6. "भुवस" शब्द में छोटा "एस" इंगित करता है कि यह एक आत्मसात "एक्स" ध्वनि है (नीचे एक बिंदु के साथ)। छोटे "यू" और "एफ" क्रमशः पिछली ध्वनि के स्वर और ओवरटोन को दर्शाते हैं।
7. अक्षर के नीचे एक बिंदु के साथ "X", तथाकथित। विसर्गा, जिसका उच्चारण यूक्रेनी "जी" या मोटे रूसी "जी" की तरह होता है, जैसा कि "अहा" शब्द में होता है।
8. अक्षर के नीचे एक बिंदु के साथ "एच", तथाकथित। सेरेब्रल "एन" (अन्य सेरेब्रल की तरह: टी, टीएक्स, डी, डीएक्स) का उच्चारण जीभ की नोक को पीछे मोड़कर किया जाता है, और जीभ का निचला हिस्सा तालु को छूता है।
9. अक्षर के नीचे एक बिंदु वाला "M" एक नासिका ध्वनि "m" है। "एनजी" के साथ संयोजन में अंग्रेजी नाक "एन" के समान; नाक में लंबी आवाज़ आती है, जैसे "एम" और "एन" के बीच कुछ।
जप का अभ्यास शुरू करने से पहले, आपको सबसे पहले मंत्र को (सही स्वर और उच्चारण के साथ) याद करना होगा, उसमें प्रत्येक शब्द के अर्थ के साथ-साथ उसके संपूर्ण अर्थ को समझना होगा।
हालाँकि, जिस स्वर के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसके लिए अन्य विकल्प भी हैं। कैसेट संग्रह "सुंदरम साईं भजन" के कैसेट वी. 10 (बी. 1.4) की रिकॉर्डिंग पर, इस मंत्र का उच्चारण वैदिक भजनों के मानक स्वर के साथ किया जाता है, जो साईं बाबा के उच्चारण के तरीके से कुछ अलग है। शब्द "सवितुर" में अक्षर "सा" के अपवाद के साथ, जिसका उच्चारण मुख्य स्वर से दो अर्धस्वर ऊपर होता है, सभी उच्च अक्षरों का उच्चारण एक अर्धस्वर अधिक होता है, और मुख्य स्वर के सापेक्ष सभी निचले अक्षरों का उच्चारण दो अर्धस्वर नीचे होता है। अत: मन्त्र की मुख्य कुंजी -

गायत्री मंत्र का जाप करने से कई सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यह शरीर, सूक्ष्म नाड़ियों, मन को शुद्ध करता है; ऊर्जा, शक्ति, स्वास्थ्य देता है; खतरे से बचाता है, कर्म ऋणों को दूर करता है, सत्व गुण को बढ़ाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंत्र हमारे मन (बुद्धि) को उत्तेजित और प्रबुद्ध करता है, ज्ञान, बुद्धि देता है और विवेक की क्षमता को बढ़ाता है। साईं बाबा कहते हैं, "जिस तरह उगते सूरज की किरणें अंधेरे को दूर कर देती हैं, उसी तरह गायत्री मंत्र का जाप अज्ञान के अंधेरे को दूर कर देता है।" उचित अभ्यास से, गायत्री हमें आत्मज्ञान दे सकती है और परम मुक्ति की ओर ले जा सकती है।
साईं गायत्री मंत्र
ऊपर वर्णित प्रसिद्ध वैदिक गायत्री मंत्र, जिसकी पूजा का उद्देश्य हमारे सौर मंडल के केंद्रीय देवता, सूर्य नारायण या सवितार हैं, गायत्री नामक मंत्रों के वर्ग में से केवल एक है।
इस मंत्र का आकार, इसकी संरचना और अर्थ विभिन्न देवताओं, या अधिक सटीक रूप से, एक भगवान (विष्णु, रुद्र, दुर्गा, आदि) के पहलुओं को समर्पित गायत्री मंत्रों की एक पूरी श्रृंखला के लिए प्रोटोटाइप के रूप में कार्य करता है। सामान्य शब्द जो इन मंत्र-प्रार्थना के सार को परिभाषित करते हैं वे हैं: "विद्महे" ("हम जानते हैं, महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं"), "धीमहि" ("ध्यान करें, हमारे विचारों को केंद्रित करें") और "प्रचोदयात्" ("यह प्रकाशित हो सकता है") ! यह आत्मज्ञान प्रदान करे!")।
ऐसा ही एक मंत्र श्री सत्य साईं बाबा को समर्पित है:
ॐ सैश्वराय विद्महे
सत्यं देवाय धीमहि
तं नः सर्वः प्रचोदयात्
ॐ! हमें एहसास है कि साईं स्वयं भगवान हैं। हम सत्यदेव का ध्यान करते हैं। वह हमें आत्मज्ञान प्रदान करें!
इस मंत्र का उच्चारण सबसे पहले वैदिक विद्वान श्री गंडिकोटा सुब्रमण्य शास्त्री ने किया था, एक व्यक्ति जिन्हें साईं बाबा महर्षि कहते थे। यह एक पवित्र दिन (24 दिसंबर, क्रिसमस की पूर्व संध्या 1977), एक पवित्र समय (सूर्यास्त के समय), एक पवित्र स्थान (बैंगलोर के पास बृंदावन आश्रम) में, पवित्र उपस्थिति में और साईं बाबा की प्रेरणा से हुआ। इस मंत्र को श्री सत्य साईं गायत्री कहा जाता है।
मंत्र की संरचना, अर्थ और उद्देश्य
साईं गायत्री मंत्र की संरचना अन्य गायत्री मंत्रों के समान है और इसमें 24 अक्षर हैं, जो 8 अक्षरों की तीन पंक्तियों में विभाजित हैं। संख्यात्मक रूप से, मंत्र में शामिल ध्वनियों की संख्या का योग पवित्र संख्या 108 है, जो दिव्य अनुग्रह की ऊर्जा के अनुरूप है।
अन्य गायत्री मंत्रों की तरह, साईं गायत्री में भी तीन भाग होते हैं। मंत्र के प्रथम भाग में - सैश्वराय विद्महे- पूजा व्यक्त की जाती है और पूजा की वस्तु (देवता) की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, इस मामले में साईं बाबा, जिनकी इस मंत्र में पहचान स्वयं ईश्वर से की जाती है। इस पंक्ति का अर्थ है: "हमें एहसास होता है (मानते हैं, जानते हैं) कि साईं स्वयं भगवान (ईश्वर) हैं।"
दूसरा हिस्सा - सत्यं देवाय धीमहि- इस बात पर जोर देता है कि एकाग्रता (ध्यान) का उद्देश्य भगवान है, जिसका नाम और सार सत्य (सत्य) है। इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है: "हम भगवान का ध्यान करते हैं, जिसका नाम सत्य है।"
तीसरा भाग - तं नः सर्वः प्रचोदयात्एक प्रार्थना है जिसका अर्थ है: "वह हम सभी को आत्मज्ञान प्रदान करें!"
जो प्राणी साईं गायत्री मंत्र की पूजा की वस्तु के रूप में प्रकट होता है, वह स्वयं भगवान है, जो श्री सत्य साईं बाबा के अवतार के रूप में मानव रूप में अवतरित हुआ है। उनके अपने शब्दों में, सत्य साईं बाबा शिव और शक्ति दोनों के अवतार हैं। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि साईं गायत्री मंत्र पहली बार लोगों के सामने सूर्यास्त के समय, शाम की संध्या के दौरान प्रकट हुआ था, जिस पर रुद्र का शासन है, जो शिव के अवतारों में से एक है। शारीरिक रूप होने के कारण, एक अवतार के रूप में सत्य साईं बाबा इस मामले में स्वयं देवता और उसकी शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मंत्र जप का उद्देश्य एवं प्रभाव
किसी भी गायत्री साधना (गायत्री मंत्र का जाप करने का आध्यात्मिक अभ्यास) का लक्ष्य देवता की शक्ति को जगाकर और अंततः उनसे दिव्य कृपा प्राप्त करके उनके साथ संचार का एक चैनल स्थापित करना है। ऐसी स्थिति में जब एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी मंत्र का जाप किया जाता है, तो देवता, यदि ऐसा कोई चैनल स्थापित किया गया है, तो इच्छा पूरी कर सकते हैं। यदि मंत्र-साधना बिना किसी अहंकारपूर्ण इच्छा के की जाए तो परिणाम स्वरूप ईश्वर की चेतना से मिलन होगा। इस प्रकार, साईं बाबा की छवि पर एकाग्रता के साथ साईं गायत्री मंत्र को दोहराने का उद्देश्य सर्वोच्च चेतना (शिव) की शक्ति को जागृत करना और उनके साथ अंतिम मिलन है। इस स्थिति में साधक की चेतना शुद्ध चेतना - शिव चेतना का रूप धारण कर लेती है। अधिक सटीक रूप से कहें तो, शुद्ध चेतना का रूप किसी भी रूप की शक्ति के समान पूर्ण निराकार है। पूर्ण निराकारता बौद्धों की शून्यता या शून्यता है। इसके पीछे केवल सार्वभौमिक पूर्णता, अर्थात् पूर्ण या परब्रह्म ही खड़ा है।
मंत्र साधना का पूरा प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि देवता के साथ एक ऊर्जा चैनल स्थापित है या नहीं, साथ ही इस चैनल की ताकत पर भी निर्भर करता है। चैनल जितना मजबूत होगा, साधक पर उतनी ही अधिक दैवीय कृपा स्वतः प्रवाहित होगी।
देवता के साथ एक ऊर्जा चैनल की स्थापना तीन मुख्य कारकों पर निर्भर करती है: ए) भावनाएँ और भावनाएँ बी) मन और सी) साधना करने वाले की इच्छा। भावनाएँ और भावनाएँ जितनी ऊँची होंगी, पूजनीय वस्तु के प्रति समर्पण की भावना जितनी मजबूत होगी, ऐसा चैनल स्थापित करना उतना ही आसान होगा। साधक का मन जितना शुद्ध होगा, वह उतनी ही अधिक दिव्य तरंगों का अनुभव कर सकेगा। देवता पर उसकी एकाग्रता जितनी मजबूत होगी, चैनल की स्थापना की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आंतरिक संकल्प जितना मजबूत होगा और जितना अधिक प्रयास किया जाएगा, चैनल उतनी ही जल्दी स्थापित हो जाएगा। कभी-कभी इनमें से एक भी कारक, बहुत कम समय के लिए भी प्रकट होकर, देवता के साथ संबंध स्थापित करने के लिए काफी होता है। यदि ये तीनों कारक मौजूद हैं, तो परिणाम अपरिहार्य है।
ऐसा चैनल देवता (भक्ति) के प्रति प्रेम और समर्पण की मजबूत भावना के माध्यम से सबसे आसानी से स्थापित किया जाता है। हालाँकि, यह चैनल भी कम स्थिर है। जब अवतार स्वयं, लोगों के बीच मानव रूप में मौजूद होता है, पूजा का पात्र बन जाता है, तो यह साधक को प्रेम (भक्ति) के माध्यम से ईश्वर के साथ एक ऊर्जावान संबंध स्थापित करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह वह रूप है जो प्रेरित करने में सबसे सक्षम है। प्यार।
मानसिक चैनल को स्थापित करना अधिक कठिन है, हालाँकि यह अधिक स्थिर हो सकता है। जो साधक बुद्धि के माध्यम से ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि ईश्वर की चेतना के साथ एकता प्राप्त करना अंततः किसी की अपनी चेतना की स्थिति में परिवर्तन मात्र है। साधक चेतना और भगवत् चेतना का शुद्ध स्वरूप एक ही है। इस अर्थ में, भगवान या साईं बाबा, उनके दृश्य अवतार के रूप में, हर किसी के भीतर हैं।
जिन लोगों को पिछले अवतारों में उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियाँ मिली हैं, वे केवल शुद्ध इच्छाशक्ति के माध्यम से अपने सर्वोच्च सार के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो साईं बाबा के वास्तविक सार से अलग नहीं है।
साईं गायत्री मंत्र को दोहराने से शास्त्रीय सविता गायत्री का पाठ करने जैसा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है: यह मंत्र बुद्धि आदि की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, प्रबुद्ध करता है और अंततः अवतार की कृपा से मुक्ति की ओर ले जाता है।
मंत्र साधना
मंत्र जप के अभ्यास में 3 घटक शामिल होते हैं: देवता, साधक और स्वयं मंत्र। इस अभ्यास का प्रभाव इन तीन घटकों की शक्तियों की परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। साधक पर प्रवाहित होने वाली देवता की शक्ति पहले से ही सही अभ्यास का परिणाम है। एक साधक की शक्ति, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसकी भावनात्मक, मानसिक और स्वैच्छिक आकांक्षा पर निर्भर करती है। मंत्र में (प्रार्थना के विपरीत) भी एक निश्चित शक्ति होती है, जिसे उचित परिस्थितियों में जागृत किया जा सकता है।
किसी मंत्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए अर्थात उसे "पुनर्जीवित" करने के लिए सबसे पहले आपको उसका सही उच्चारण करने में सक्षम होना चाहिए। उत्तरार्द्ध मानता है कि ध्वनियों का उच्चारण (उनके देशांतर सहित), तनाव और विराम का वितरण, साथ ही इसका स्वर सही होना चाहिए। लयबद्ध पुनरावृत्ति एक अतिरिक्त ऊर्जा आवेग पैदा करती है जो संचयी प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात, प्रत्येक बाद की पुनरावृत्ति के साथ एक दूसरे पर समान तरंगों के सुपरपोजिशन के कारण। स्वरों में वैकल्पिक परिवर्तनों के प्रभाव से कुछ कंपन भी उत्पन्न होते हैं जो स्वयं देवता की ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जिसके लिए मंत्र बाहरी आवरण है।
साईं गायत्री मंत्र के अभ्यासियों के लिए, नीचे हम इसके स्वर चिह्न प्रस्तुत करते हैं, जो "सुंदरम साईं भजन" संग्रह के कैसेट वी: 5 (ए 4.8) पर रिकॉर्डिंग के अनुसार बनाए गए थे। यह मंत्र शास्त्रीय वैदिक स्वर के साथ उच्चारित किया जाता है और इसमें एक कुंजी होती है। इसका मतलब यह है कि मुख्य स्वर के संबंध में जो शब्दांश ऊंचे हैं, उनका उच्चारण 1 सेमीटोन अधिक (+1) किया जाता है, और सभी निचले अक्षरों का उच्चारण 2 सेमीटोन कम (-2) किया जाता है। अन्य विशेषक शास्त्र के डिकोडिंग के लिए, गायत्री मंत्र के उच्चारण की व्याख्या देखें।

साईं गायत्री मंत्र का जाप सुबह और शाम के समय सबसे अच्छा किया जाता है। यदि गायत्री मंत्र का प्रभाव सुबह की संध्या के दौरान सबसे शक्तिशाली माना जाता है, तो साई गायत्री का पाठ करने का प्रभाव, रुद्र-शिव के साथ इसके रहस्यमय संबंध के कारण, शाम की संध्या के दौरान अधिक शक्तिशाली होने की संभावना है (जब यह पहले पाठ किया जाता है)। हालाँकि, इसे किसी भी समय, किसी भी स्थिति में दोहराया जा सकता है: भोजन से पहले, स्नान के दौरान, खतरे की स्थिति में, आदि।
इसे कम से कम 3 बार या यदि समय मिले तो 10 बार दोहराया जाना चाहिए। इसे 108 बार दोहराना सर्वोत्तम है। इस स्थिति में, दैवीय कृपा की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। एकमात्र संख्या जो इसके वाहक के रूप में कार्य करती है वह संख्या 108 है। इस ऊर्जा को समझने के लिए, आपको इसके प्रति पूरी तरह से खुला होना होगा। अन्यथा, यह ऊर्जा अप्रयुक्त अपने स्रोत पर लौट आती है। इसीलिए, जप (मंत्र जाप) के बाद, साथ ही दर्शन के बाद, साईं बाबा कम से कम एक संक्षिप्त ध्यान की सलाह देते हैं ताकि साधक दिव्य कृपा की ऊर्जा को आत्मसात कर सके।
साईं गायत्री मंत्र को ज़ोर से दोहराने का अभ्यास शुरू करना सबसे अच्छा है। बाद में आप इसे मानसिक रूप से दोहराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसका अभ्यास गायत्री मंत्र की तरह ही किया जाना चाहिए, जिसमें दृश्य में गायत्री देवी की छवि (चमकदार सर्कल के केंद्र में) को साईं बाबा की छवि से बदल दिया जाना चाहिए।
साई गायत्री के अन्य रूप
उपरोक्त प्रसिद्ध साईं गायत्री मंत्र के अलावा, इसके अन्य रूप भी हैं, उदाहरण के लिए: "साईं रामाय विद्महे, आत्मा रामाय धीमहि, तन्नो बाबा प्रचोदयात्!" "हम साईं को शुद्ध आनंद के स्रोत के रूप में महसूस करते हैं! हम साईं पर ध्यान करते हैं, जो हमारा उच्च स्व (आत्मान) है! वह हमें आत्मज्ञान प्रदान करें!" लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध वह संस्करण है जिसके बारे में डायना बास्किन ने अपनी पुस्तक "डिवाइन मेमोरीज़" में लिखा है:
ॐ! हमें एहसास होता है कि सत्य स्वयं भगवान है। हम पार्टी से प्रभु का ध्यान करते हैं। साईं हमें ज्ञान प्रदान करें!
जैसा कि डायना बास्किन गवाही देती हैं, यह मंत्र (अधिक विस्तारित पहली पंक्ति के साथ: "ओम! श्री सत्य साईं देवाय ...") एक बार एक महिला को सपने में दिया गया था जो नहीं जानती थी कि यह क्या था। एक दर्शन में, उसने खुद को डायना बास्किन की माँ के बगल में पाया और एक कागज के टुकड़े पर मंत्र का पाठ लिखकर, इस मंत्र के बारे में उनकी राय पूछी। उसी समय साईं बाबा उनके पास आये। उन्होंने कागज का टुकड़ा लिया और उसे देखकर कहा: “यह साईं गायत्री है। यह कहना। यह एक अच्छा मंत्र है।"
जैसा कि हम देखते हैं, अपने अर्थ में साईं गायत्री का यह संस्करण रूढ़िवादी संस्करण से भिन्न नहीं है, हालाँकि एक ही अर्थ थोड़े अलग शब्दों में व्यक्त किया गया है। शायद, छंदबद्ध और गूढ़-संख्यात्मक अर्थ में, यह मंत्र रूढ़िवादी साईं गायत्री से भिन्न है, लेकिन साईं बाबा के सच्चे अनुयायी के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। इस मंत्र के प्रभाव की पुष्टि स्वयं डायना बास्किन और इसका अभ्यास करने वाले साईं बाबा के कई अन्य अनुयायियों ने की है।
शांति शांति शांति
श्री सत्य साईं बाबा का खेरसॉन केंद्र। बी ० ए। ज़ागोरुल्को. गायत्री और साई गायत्री मंत्र. संपादक: एन.एन. सैमसोनोवा। "साई वेद" - खेरसॉन, 1997।
गायत्री मंत्र एक ऐसा उपकरण है जो आपको आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की अनुमति देता है। दैनिक अभ्यास से, यह आपको जीवन शक्ति से रिचार्ज करने और आवश्यक प्रवाह को अपनी ओर आकर्षित करने की अनुमति देता है।
कर्म शुद्धि हेतु प्रार्थना
मंत्र में उनके जीवन को बदलने की शक्ति है। हालाँकि सबसे लोकप्रिय प्रार्थनाओं में से एक, इसके बारे में शायद सभी ने सुना होगा। गायत्री मंत्र अभ्यासकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन उपयोग किया जाने वाला एक सार्वभौमिक उपकरण है।

ऐसे गानों की बदौलत व्यक्ति सौर ऊर्जा की ओर रुख कर सकता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी प्रशंसाएँ और प्रार्थनाएँ होती हैं, उदाहरण के लिए,।
गायत्री बुरे विचारों, अनावश्यक जानकारी से मुक्ति दिलाती है, दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से बचाती है और कर्म को रीसेट करती है। दैनिक अभ्यास से आप संसार अर्थात निरंतर पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल सकते हैं।
चक्र को छोड़कर आप स्वयं को एक नई दुनिया में पाते हैं। ख़ासियत यह है कि पिछले सभी जन्म भुलाए नहीं जाते हैं, और व्यक्ति अपने संचित अनुभव के साथ रहता है।
आध्यात्मिक गुरुओं ने दावा किया कि गायत्री मंत्र सबसे शक्तिशाली है। जब उन्हें जरूरत महसूस होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भोजन से पहले, कुछ जल प्रक्रियाओं के दौरान। प्रार्थना का जाप करके व्यक्ति स्वयं को और अपने साथ-साथ अपने आस-पास के स्थान को भी शुद्ध करता है। मंत्र को 108 बार पढ़ा जाता है।अभ्यासकर्ताओं का कहना है कि इस तरह आप भगवान ब्रह्मा की सर्वोच्च पत्नी - देवी गायत्री के करीब पहुंच सकते हैं।